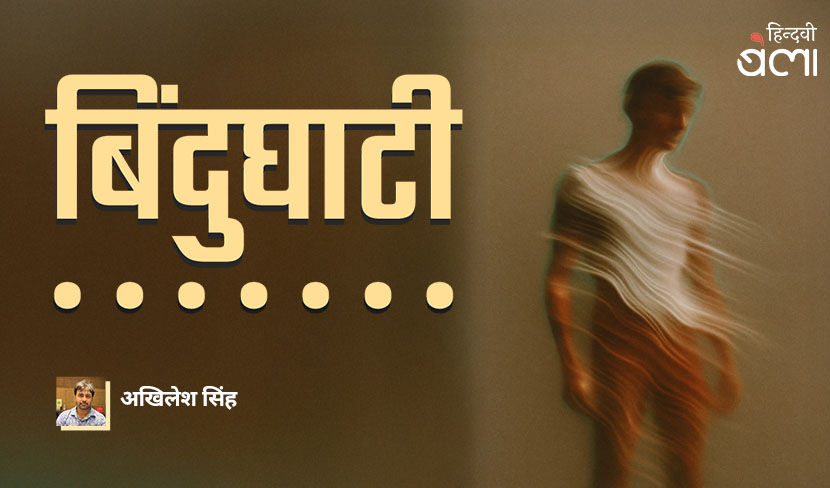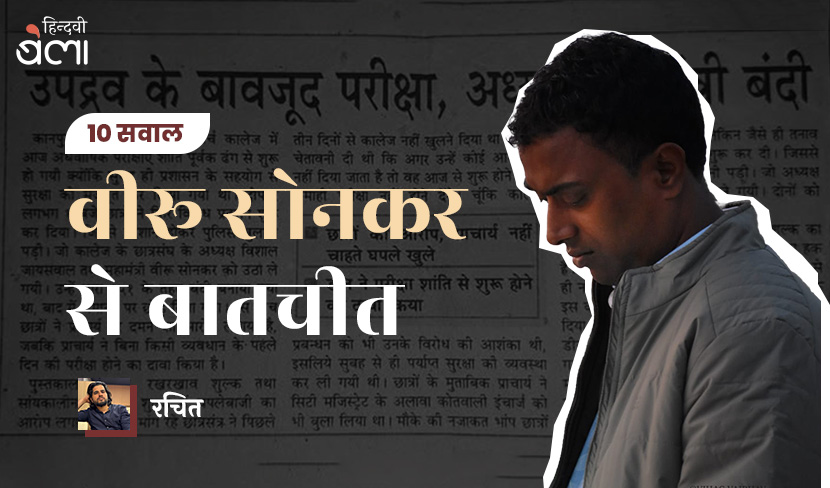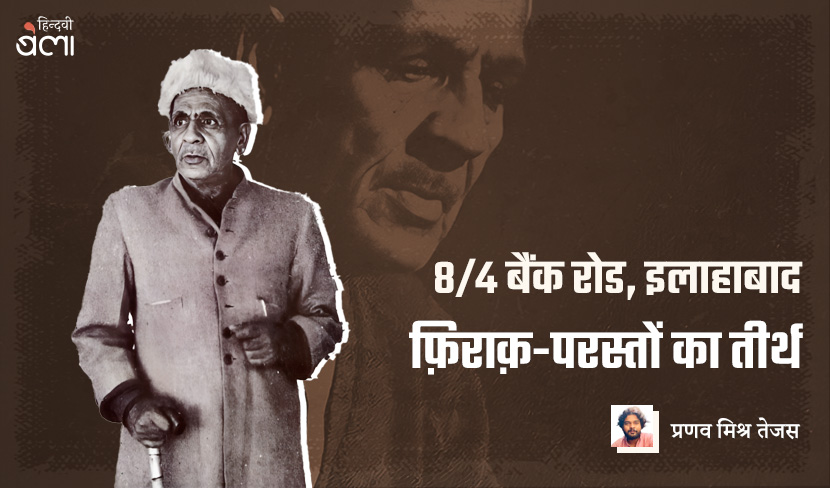राग गांधी मल्हार वाया तीस जनवरी मार्ग
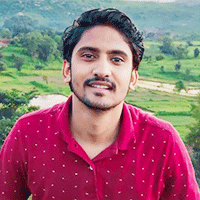 पीयूष तिवारी
22 जुलाई 2024
पीयूष तिवारी
22 जुलाई 2024

वह मुख—अरे, वह मुख, वे गांधी जी!!
— मुक्तिबोध
दुर्घटनाग्रस्त सड़कों, जननायक-रिहाई-केंद्रित धरना-प्रदर्शनों के बीच (कु)भाषणों और पाँच वर्षों में एक बार आने वाले लोकतंत्र के महापर्व की उत्सवधर्मिता समाप्त हो चुकी थी। विमर्शों की टूटी टाँग लिए जनवादी सीमापुरी से होते हुए मध्य दिल्ली में घुसपैठ को आतुर थे। यह वही वक़्त था, जब साल भर टर्राने वाले मेढ़कों में ज़ुकाम की शिकायत बढ़ रही थी।
आम भारतीय शहरों की तर्ज़ पर कनॉट प्लेस में खड़े खलिहर तमाशबीन—‘भैयाजी कहीन’ जैसे फूहड़, सत्तापोषित, उन्मादी-शो की ग़ैर-ज़रूरी बहसों में ख़ुद को स्थापित करने पर आमादा थे।
विश्वविद्यालयों में गर्मी इस क़दर उत्कर्ष पर थी कि उनका पतन—शीघ्रपतन से भी शीघ्र हो सकता था। अपनी दोग़ली नीतियों, हिंदी विभाग से अन्यमनस्क की भावना—किसी बंगाली बाबा के चूरन के इस्तेमाल के उपरांत भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी।
गुप्त रोग के विज्ञापन सरीखे विश्वविद्यालयी मीटिंग के इश्तिहार पूरी दिल्ली में चस्पाँ थे। वाइस चांसलर आसमान-आसमान चलने की ख़ुदयक़ीनी में मुब्तला थे और धरती नापने जैसी बातों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी।
विश्वविद्यालयों में प्रेम ढूँढ़ने वालों की जगह आरक्षित हो रही थी। चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी में खड़ा पुतला किसी तानाशाह की याद दिला रहा था, जो मधुमेह की तरह सामान्य आत्ममुग्धता से गोह की तरह अपनी जगह पर चिपका बैठा था—कितना भी छेड़ो, दुरदुराओ, अपनी जगह से टस से मस नहीं।
वह साँपों के बीच गेहुँअन और लोगों में होरहोरवा हो जाना चाहता था। इस नृशंस शहर में आग इतनी थी कि अपनी कविता में कोई भी मुक्तिबोध—‘बेहतरी की ख़ोज में ख़ुद को झुलसाने में अशक्त था।’
राजधानी में धर-पकड़ की सुनियोजित कार्रवाई, इलेक्टोरल बॉन्ड की ख़बरों, अति सामान्य हो चुके हत्या-बलात्कार जैसे (कु)कृत्यों की ऊहापोह के बीच—‘तीस जनवरी मार्ग’ स्थित ‘गांधी स्मृति’ जाना हुआ।
चारों तरफ़ सरकारी अभिजात्य का दख़ल था। पूँजीपति के.के. बिरला द्वारा घर के साथ बेचे गए पेड़ों पर बैठे पंछियों की ध्वनि में ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए’ की धूम इतनी थी कि—परिसर में फैले गांधी जी के महात्म्य को अलग से रेखांकित करने की ज़रूरत नहीं मालूम हो रही थी। सब कुछ सुरम्य, सब कुछ शांत—ठीक अभी-अभी हत्या के बाद वाली ख़ामोशी।
प्रवेश-द्वार पर स्थित शिल्पकार ‘श्री राम सुतार’ कृत गांधी जी की मूर्ति के ठीक नीचे सुंदर अक्षरों में लिखा था—‘मेरा जीवन ही मेरा संदेश है’। हालाँकि गांधी जी ने यह कहते हुए कभी नहीं सोचा होगा कि—वह विचारों से ज़्यादा स्मारकों में पाए जाएँगे। पक्की इमारतें उनकी स्मृति कम प्रदर्शनी ज़्यादा लगेगी—जो देश-विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए लहालोट होने और सरकारी तंत्र हेतु आँकड़ों में इज़ाफ़ा पाने का कारण बनेगी।
लोक के फ़र्ज़ी लालित्य से संक्रमित, उबाऊ और कामचलाऊ गाइड ने सर्वप्रथम हमारे सम्मुख समूचे परिसर का कु-पठित आधा-अधूरा ब्योरा प्रस्तुत किया। यह इतना औसत था कि इसे सुनकर दृश्य परंपरा से अपरिचित सूरदास भी नक़्शे पर घाव के पठार बड़ी आसानी से पहचान सकते थे।
उनकी जानकारी इतनी रोमांचक और सुपाच्य थी कि हर सुनने वाला जूते की नोक से ज़मीन में चार फ़ीट गहरा गड्ढा खोद सकता था। अपनी लुका-छुपी प्रतिभा से अनजान खड़े लोगों को देख कर यह साफ़ ज़ाहिर था कि ‘खोदने का निर्वाण’ सिर्फ़ प्राचीन संस्कृति की खोज करने वाले शोधकर्ताओं को ही नहीं, आम जनों को भी प्राप्त है।
इस बात से लगभग संतुष्ट-सत्ताधारियों द्वारा पूजित—‘हत्यारे’ का नाम लिए बिना बड़ी ही चतुराई से उन्होंने मानव हत्या की समूची घटना को अपनी चहलकदमी में निपटा दी। अपनी गौरवपूर्ण उपलब्धि पर उनकी उग आई मंदस्मिति इस बात की तस्दीक़ कर रही थी—अगर लोमड़ियों के सिंग होते तो वे बारहसिंगा होतीं।
चलने से धैर्य आता है और संगीत सुनने से त्रासदी कम होती है। वह कौन-सी त्रासदी थी—जिसने कुमार गंधर्व को मजबूर किया होगा ‘राग गांधी मल्हार’ रचने के लिए। वह कौन-सी बे-हयाई थी—जो सत्य-अहिंसा-सत्याग्रह जैसे शब्दों में उन जैसों की उपस्थिति सुनिश्चित कर रही थी। उन्माद भरे इस समय में यह चमत्कृत करने वाली बात हो सकती है मगर भीतर समाहित करने के क्रम में एक चमक में विलीन भी।
इस पिघलती हुई भयावह दुपहरी से आजिज़ होकर प्रतिरोध की शक्ल में हमारे पास कुछ नहीं था―सिवाय तंबाकू रगड़ने के अभिनय में गदौरी मलने के। हर रगड़ के बाद की थाप दांडी मार्च वाली बकरी की लेंड़ी की ताज़ा गंध आब-ओ-हवा में घुल रही थी। शहर में धूल उड़ रही थी और इस क़दर उड़ रही थी जैसे ज़मीन ही ख़त्म हो जाएगी।
पसीने की बदबू बता रही थी कि हर देह के भीतर एक नमक का सत्याग्रह था और हर मेहनतकश देह को तोड़कर नमक बनाया जा सकता था। अब कोई भी औसत आदमी किसी हिंदी-कवि का रूमानी अंदाज़ अख़्तियार कर कह सकता था—
तुम्हारी देह ने एक देह का
नमक खाया है।
— केदारनाथ सिंह
‘सुमना’ के सामने स्थित ‘विश्व शांति घंटा’ पर इजरायल का झंडा है और फ़िलिस्तीन अब भी कहीं कोने में बैठा विलाप कर रहा था। वहाँ उपस्थित अधिकारियों-पदाधिकारियों से सुमना, गांधी, हत्यारे इत्यादि केंद्रित किसी भी जिज्ञासा के बदले, फुसफुसाहटों के अलावा कुछ सुनाई देना जैसे विरल था।
इस आधार पर यह प्रमाणित था कि सामूहिकता की शक्ति उनमें काफ़ी मात्रा में मौजूद थी—निरुत्तर होने की स्थिति में वे आंदोलन-जैसा कुछ छेड़ सकते थे। माकूल जवाब न मिलने की स्थिति में यह सुनिश्चित हुआ कि उन्हें अपच की शिकायत है और समूचे देश का पेट ख़राब हो रहा था।
सब कुछ निपटने के दौरान की सामान्य मगर ज़रूरी बातचीत में एक उदारवादी प्रोफ़ेसर ने बड़े ही आर्द्र स्वर में करुणा न उपजाने के उद्देश्य से कहा—‘उनके दौर में यह जगह ऐसी नहीं हुआ करती थी।’
बात ठीक भी है। मगर विश्वविद्यालयों में स्थायी प्रोफ़ेसरों की एक बात बड़ी निराली होती है कि उनका दौर दूसरों के दौर से हमेशा अधिक प्रगतिशील होता है। मसलन उनके दौर में रिश्वत, रिश्वत नहीं एक कनस्तर घी थी, भ्रष्टाचार जेल का नहीं मुक्ति-द्वार था, कुछ सूक्तियाँ—चाक़ू चलाने की नहीं घोंपने की चीज़ है, तमंचा दिखाने की नहीं चलाने की चीज़ है।
समझ नहीं आता कि उनका दौर रेंड़ी (अरंडी) के तेल में बना था कि साँडे के तेल में। वैसे भी अब कौन ‘रिस्क है’ की तर्ज़ पर जोख़िम उठाए और ललकार कर कहे—वे दिन लद गए प्रोफ़ेसर, वे दिन लद गए।
एक व्यवस्थित कमरे की सबसे बड़ी दुर्गति उसका अति-व्यवस्थित होना है। यहाँ आने वालों के लिए मुख्य गेट पर चस्पाँ होना चाहिए—‘बिखराव में सौंदर्य’ खोजने वालों के हाथ सिर्फ़ निराशा लगेगी।
यह कौन-सी स्मृति है, जहाँ स्मरण के आलोक में बहुधा सुंदरता ही सुंदरता है—जबकि होने को एक विद्रूपता तक नहीं। यह कौन-सी स्मृति है, जहाँ पूर्ववर्तियों की उपस्थिति अपनी प्रतिष्ठा खोती हुई हास्यास्पद होती जा रही है और इस महान जगह की महानता इसे और विपन्न कर रही!
यह कौन-सी स्मृति है, जहाँ अतीत का महुआ नहीं टपकता और चौथी गोली की ठाएँ अब भी किसी म्यूजियम की पिस्तौल में क़ैद है।
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
12 जून 2025
‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही’
‘बॉर्डर 2’ का विचार सुनते ही जो सबसे पहला दृश्य मन में कौंधा, वह बालकनी में खड़े होकर पिता का कहना था—‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही।’ इस वाक्य में सिर्फ़ एक अभिनेता का अवसान नहीं था, एक पूरे युग क
29 जून 2025
‘बिंदुघाटी’ पढ़ते तो पूछते न फिरते : कौन, क्यों, कहाँ?
• उस लड़की की छवि हमेशा के लिए स्टीफ़न की आत्मा में बस गई, और फिर उस आनंद में डूबा हुआ पवित्र मौन किसी भी शब्द से नहीं टूटा... आप सोच रहे होंगे कि यहाँ किसी आशिक़ की किसी माशूक़ के लिए मक़बूलियत की बा
14 जून 2025
बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल!
‘बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल’—यह नब्बे के दशक में किसी पल्प साहित्य के बेस्टसेलर का शीर्षक हो सकता था। रेलवे स्टेशन के बुक स्टाल्स से लेकर ‘सरस सलिल’ के कॉलमों में इसकी धूम मची होती। इसका प्रीक्वल और सीक्वल
10 जून 2025
‘जब सोशल मीडिया नहीं था, हिंदी कविता अधिक ब्राह्मण थी’
वर्ष 2018 में ‘सदानीरा’ पर आपकी कविता-पंक्ति पढ़ी थी—‘यह कवियों के काम पर लौटने का समय है’। इस बीच आप फ़्रांस से लौटकर आ गए। इस लौटने में काम पर कितना लौटे आप? 2018 में जब यह कविता-पंक्ति संभव हुई
20 जून 2025
8/4 बैंक रोड, इलाहाबाद : फ़िराक़-परस्तों का तीर्थ
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एम.ए. में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी मेरे मित्र बन गए। मैं उनसे उम्र में छोटा था, लेकिन काव्य हमारे मध्य की सारी सीमाओं पर हावी था। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। उनका नाम वीरेंद्र