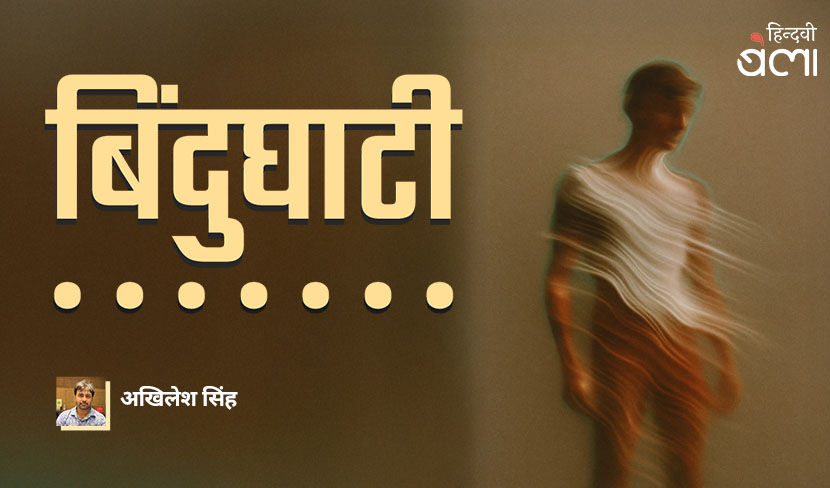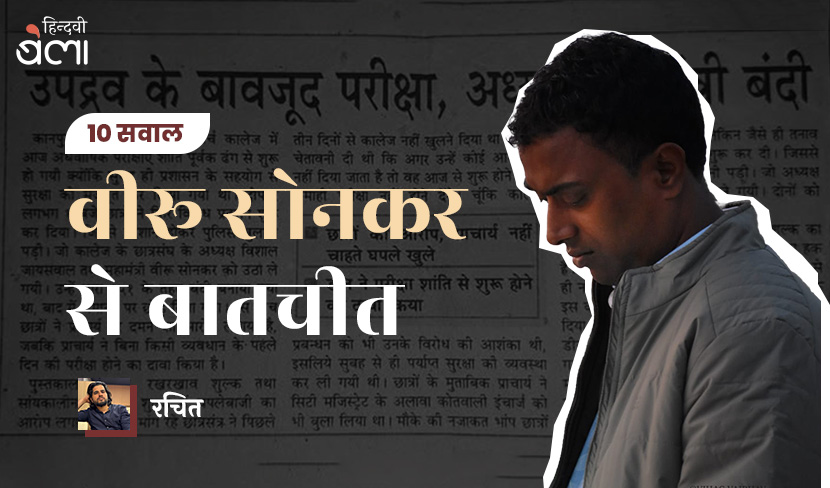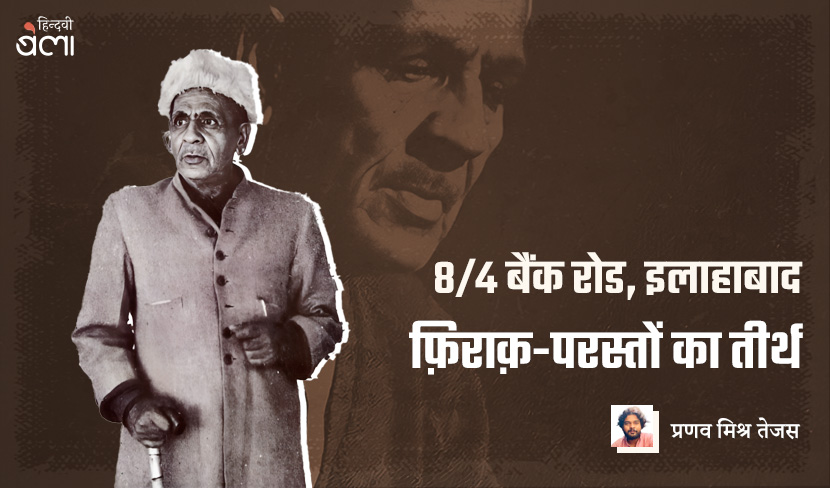अनुभूति की शुद्धता का सवाल
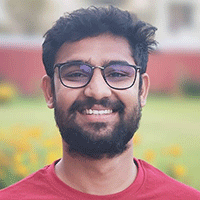 योगेश शर्मा
08 मार्च 2025
योगेश शर्मा
08 मार्च 2025

अभी कुछ दिन हुए एक साथी कहता था कि यार कुछ भी कहो कविताओं के जो अर्थ फ़लाँ आलोचक निकाल कर गए हैं, ऐसे कविता को समझना आज के पाठक के बूते के बाहर है। मैंने कहा कि पाठक ही क्यों ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में कविता को समझना तो आज के आलोचक के भी बस में नहीं। वह कुछ झल्ला-सा गया। शायद उसे किसी दूसरी तरह के जवाब की उम्मीद थी। इस डर से कि कहीं वह बातचीत को इसी बिंदु पर छोड़कर ही ना चला जाए, मैंने ही जल्दी में बात को आगे बढ़ाया।
मैंने कहा, देखो साथी कोई भी पाठक कविता का अर्थ अपने समय की परिधि में रहकर ही ग्रहण करता है। दूसरा यह भी संभव है कि कोई आलोचक अपने वर्तमान के आधार पर भविष्य का कुछ अनुमान करके अर्थ ग्रहण करे। मैं चाहता तो न था लेकिन जबरन मुझे मुक्तिबोध का ज़िक्र करना पड़ा। मेरे साथी को मुक्तिबोध से विशेष क़िस्म की चिढ़ थी। उसका मानना था कि मुक्तिबोध निहायती अटपटी भाषा वाले एक जटिल कवि हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़लाँ आलोचक ने ही समझा है। ख़ैर, मैंने उसको कहा कि कविता का अर्थ ग्रहण करते हुए सबसे अधिक काम पाठक की संवेदना करती है और संवेदना का निर्माण...!
वह बिफर पड़ा। उसने बीच में ही मुझे रोकते हुए तपाक से प्रश्न किया—तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई ऐरा-ग़ैरा नया पाठक मुक्तिबोध को उन विद्वान और प्रतिष्ठित आलोचक से अधिक समझ सकता है? अरे भाई! उनके मरने के इतने बरस बाद भी उनकी पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं; तुम कहते हो कि व्यक्ति संवेदना से समझता है, अपने समय से समझता है—यह कोरी बकवास है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक बीड़ी निकाल कर सुलगा ली। मुझे पुनः मुक्तिबोध याद आ गए।
मैंने लगभग याचना भरे लहजे में कहा कि अगर तुम ज़रा-सी दिलचस्पी दिखाओ तो मैं अपनी बात कहूँ? उसने बहुत गंभीरता का प्रदर्शन करते हुए हल्की-सी गर्दन हिलाई और बीड़ी से राख झाड़ते हुए बोला कहो। मैंने थोड़ी देर उसके लहजे को परखा। फिर कुछ सोचकर बोला कि देखो बात ऐसे है—“फ़लाँ आलोचक ने अपने समय में जिस लेखक को पढ़ा था उसे तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से ही समझा था, अगर नए पाठकों और आलोचकों को पुराने कवियों पर बातचीत के पर्याप्त अवसर नहीं मिलेंगे तो कविता के अर्थ में नवाचार की संभावनाएँ कैसे फलित होंगी? कोई कविता कालजयी कैसे होगी? कोई कविता कैसे देशकालातीत होगी? अभिधा और व्यंग्यार्थ में कुछ तो भिन्नता होगी? शास्त्र और साहित्य में कुछ तो फ़र्क़ होता होगा? हम किसी कविता को महत्त्वपूर्ण तभी मानते हैं जब पीढ़ी-दर-पीढ़ी नए पाठक उसमें से अपने मतलब का कुछ खोज निकालें। कविता से यदि नया पाठक जुड़ाव ही महसूस नहीं कर पाया तो फिर कविता के कविता होने के मायने ही क्या हैं? उसको अलग से प्रकाशित करने की या उसके पृथक पाठ की आवश्यकता क्या है? देखो यद्यपि आलोचना कविता के अर्थ में विकास करती है तथापि आलोचना जितनी पुरानी पड़ती जाती है वह उसके अर्थ में बाधक भी बन जाती है। मैं तो कहता हूँ कि कोई सजग और संवेदनशील पाठक यदि किसी महत्त्वपूर्ण रचना का पाठ बिना किसी आलोचकीय पूर्वाग्रह के करता है तो इसमें वह साहित्य पर उपकार ही करता है। कहो तुम इस बात से कुछ इत्तिफ़ाक़ रखते हो या नहीं?” मुझे लगा मैंने उससे साहित्य के सबसे गंभीर सवाल पूछ डाले हैं, इतने में वह ज़रूर घबरा जाएगा।
उसकी बीड़ी ख़त्म हो गई थी, उसने दूसरी बीड़ी लगाने के उद्देश्य से अपनी जेब में हाथ डाला। पता नहीं क्यों मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा तुम पहले इस बात को ख़त्म करो। मैंने अपने भीतर उतावलापन महसूस किया।
उसने कहा देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन क्या देश भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रोफ़ेसर कविताओं की ग़लत व्याख्याएँ करते हैं? उनकी व्याख्याओं का प्रेरणा स्रोत भी तो विद्वान आलोचकों द्वारा की गई समीक्षाएँ ही हैं। यह भी तो हो सकता है कि कोई समीक्षा ही कालजयी हो? कोई आलोचक भी तो भावी का अनुमान कर सकता है। कहो तुम्हारा इस विषय में क्या विचार है?
प्रतिउत्तर में ऐसे गंभीर प्रश्न की आशा मुझे उससे न थी। मुझे एकदम से महसूस हुआ कि मैंने उसे बीड़ी पीने से रोककर बड़ी भारी ग़लती कर दी। मैंने तो सोचा था कि आज की बातचीत में विजेता का तमग़ा मेरे हिस्से आएगा। क्षणभर को मैं कुछ सोचता रहा। फिर अनमने से भाव से मैंने बोलना आरंभ किया, “जिस विद्वान ने पहले पहल किसी कविता के अर्थ को गहराई से समझा उसने ज़रूर साहित्य पर उपकार किया, आगे के पाठकों को उसका ऋणी होना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए लेकिन साथ-ही-साथ नए पाठकों में इतना साहस तो होना ही चाहिए कि वे जब कविता का पाठ करें तो उसमें कुछ अपना निजी अर्थ भी जोड़ें। जो पुराना पड़ गया है उसे चिह्नित करें।”
मैंने उसको थोड़ी देर गार्डन में टहलते हुए बात करने को कहा लेकिन उसने एक झटके में ना कहते हुए गर्दन हिला दी। मैं मुस्कुरा दिया और आगे कहने लगा—“भाई देखो कोई गंभीर से गंभीर आलोचक भी प्रायः रचना को किसी विशेष परिप्रेक्ष्य में देखने का आदि होता है। हो सकता है कि वह विशेष दृष्टिकोण लंबे समय तक प्रासंगिक बना रहे, लेकिन उसके समानांतर यह संभावना हमेशा बनी रहती है कि उसी रचना को कोई नया पाठक बिल्कुल भिन्न ढंग से देखे। समय के बदलने के साथ देश-काल की परिस्थितियाँ बदलती हैं और उसके साथ ही नए संभावनाशील और संवेदनशील पाठक की अनुभूति में भी परिवर्तन होता है। यहाँ सवाल परीक्षा में समीक्षा लिखकर उत्तीर्ण होने का नहीं है, बल्कि अनुभूति की शुद्धता का है। यदि कविता के अर्थ में नवीनता की गुंजाइश शेष नहीं है तो फिर वह कविता प्रासंगिक नहीं रही। तुम बताओ कि आख़िर कविता प्रासंगिक कैसे बनी रहती है? (मेरे स्वर में मैंने आवेश महसूस किया।) थोड़ा ठहर कर मैंने अंतिम उद्घोष की तरह उसपर एक वाक्य फेंका—कविता के नए पाठकों को चाहिए कि वे कविता से उपजी अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करें, गढ़ें और मठों से डरे नहीं।”
उसने अपनी उँगलियाँ बालों में घुमाई और ज़बरदस्ती बात ख़त्म करने के लहजे में हामी भरते हुए कहा—हम्म!!!
मुझे लगा कि शायद इस बातचीत को इस तरह नहीं समेटा जा सकता। कोई ठोस बात कहने की कोशिश करनी होगी नहीं तो हफ़्ते भर उसके चेहरे पर यह भाव मजबूरन देखकर कुढ़ते रहना होगा कि तुमने कोशिश तो की लेकिन तुमसे बात बनी नहीं।
उसको किसी तरह दो मिनट और रोकने के लिए मैंने कहा, तुम बीड़ी क्यों नहीं सुलगा लेते? उसको जैसे कोई महत्त्वपूर्ण काम याद आ गया, जिसे वह बातों-ही-बातों में करना भूल गया हो। उसने एक बीड़ी निकाली और सुलगा ली।
मुझे मौक़ा मिल गया। मैंने कहना आरंभ किया। साथी तुम्हें देखना चाहिए कि हम दशकों-दशक एक कविता के साथ चिपके रहते हैं और लगभग एक ही तरह के अर्थ के साथ। एक ही अर्थ को, एक ही अवधारणा को उसकी प्रासंगिकता का आधार बनाकर। वही बातें अलग-अलग भाषाई मुहावरे में दोहराते रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? महान् कविता में अनंत अर्थ निहित होते हैं। मैं तुम्हें अनंत के विषय में एक कहानी सुनाता हूँ जो गणित के दर्शन में प्रसिद्ध है। यह कहानी मैंने भी कहीं सुनी थी—“एक अनंत कमरों वाला होटल है। इस होटल में हर समय कमरे ख़ाली मिल सकते हैं। इस होटल की मैनेजर बहुत होशियार है। जब भी कोई नया यात्री आता है तो वह होटल के माइक में घोषणा कर देती है कि पहले से ठहरे हुए सब यात्री एक कमरा आगे खिसक जाएँ। इस तरह हर नया यात्री पहले कमरे में ठहर सकता है। अब एक समस्या आती है। एक अनंत यात्रियों वाली बस आती है और उसके सब यात्रियों को एक-एक कमरा चाहिए। अब होटल की मैनेजर, सब पहले से ठहरे हुए सब यात्रियों के लिए घोषणा करती है कि सब यात्री अपना सामान लेकर अपने कमरे की संख्या से दुगुनी संख्या वाले कमरे में चलें जाएँ। इस तरह सारे विषम संख्या वाले कमरे ख़ाली हो जाते हैं और अनंत यात्री उस अनंत कमरों वाले होटल में आसानी से ठहर सकते हैं और यह सिलसिला अनंत समय तक चलता रह सकता है। हो सकता है इसका कोई छोर हो लेकिन वह बहुत दूर होगा।”
अब तुम इस बात को कविता पर लागू करो। कविता दरअस्ल अनंत अर्थों वाली एक इमारत की तरह है जिसमें अनंत पाठक अपनी-अपनी संवेदनाओं और ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, हर नई पीढ़ी के पाठक के लिए पहला कमरा ख़ाली कर दिया जाता है। अस्ल में कविताओं को किसी भी एक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखना उसके अनंत अर्थ को सीमित करने जैसा है जो अनंत संभावनाओं को स्वीकार करने और उसको खोजने का साहस जुटाने से बचने का एक बढ़िया बहाना है। अर्थ तो दरअस्ल सापेक्षता के संदर्भ में ही निहित होता है। वह अपने समय के साथ जुड़कर ही प्रकट होता है।
अच्छा, ठीक है। उसने बीड़ी फेंकते हुए कहा। अब मुझे जाना होगा। आज मुझे विद्यार्थियों को एक लंबी कविता का पाठ कराना है।
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
12 जून 2025
‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही’
‘बॉर्डर 2’ का विचार सुनते ही जो सबसे पहला दृश्य मन में कौंधा, वह बालकनी में खड़े होकर पिता का कहना था—‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही।’ इस वाक्य में सिर्फ़ एक अभिनेता का अवसान नहीं था, एक पूरे युग क
29 जून 2025
‘बिंदुघाटी’ पढ़ते तो पूछते न फिरते : कौन, क्यों, कहाँ?
• उस लड़की की छवि हमेशा के लिए स्टीफ़न की आत्मा में बस गई, और फिर उस आनंद में डूबा हुआ पवित्र मौन किसी भी शब्द से नहीं टूटा... आप सोच रहे होंगे कि यहाँ किसी आशिक़ की किसी माशूक़ के लिए मक़बूलियत की बा
14 जून 2025
बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल!
‘बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल’—यह नब्बे के दशक में किसी पल्प साहित्य के बेस्टसेलर का शीर्षक हो सकता था। रेलवे स्टेशन के बुक स्टाल्स से लेकर ‘सरस सलिल’ के कॉलमों में इसकी धूम मची होती। इसका प्रीक्वल और सीक्वल
10 जून 2025
‘जब सोशल मीडिया नहीं था, हिंदी कविता अधिक ब्राह्मण थी’
वर्ष 2018 में ‘सदानीरा’ पर आपकी कविता-पंक्ति पढ़ी थी—‘यह कवियों के काम पर लौटने का समय है’। इस बीच आप फ़्रांस से लौटकर आ गए। इस लौटने में काम पर कितना लौटे आप? 2018 में जब यह कविता-पंक्ति संभव हुई
20 जून 2025
8/4 बैंक रोड, इलाहाबाद : फ़िराक़-परस्तों का तीर्थ
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एम.ए. में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी मेरे मित्र बन गए। मैं उनसे उम्र में छोटा था, लेकिन काव्य हमारे मध्य की सारी सीमाओं पर हावी था। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। उनका नाम वीरेंद्र