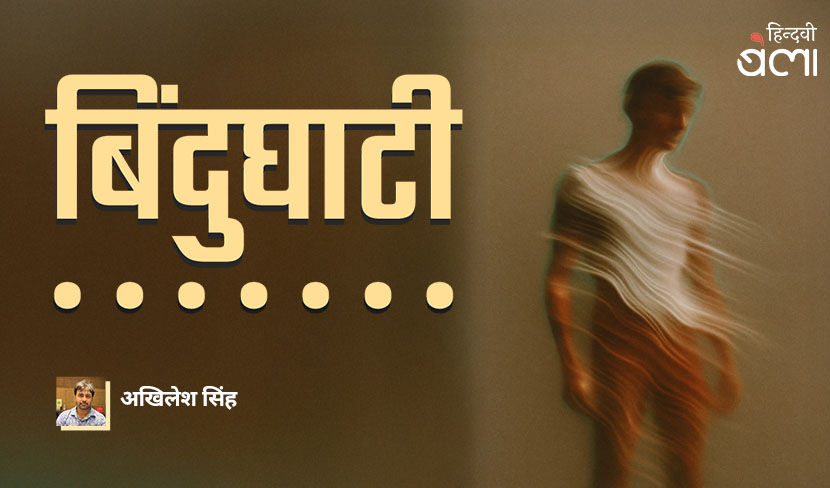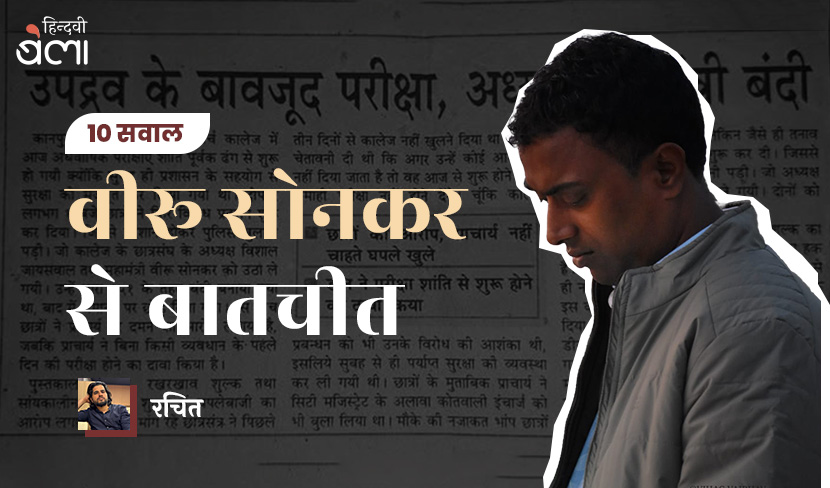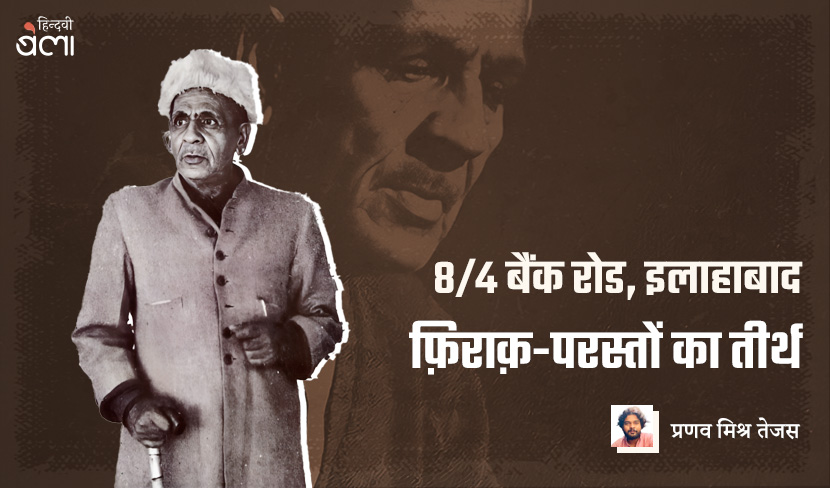यात्रा के बाद यात्रा-वृत्तांत से हटकर
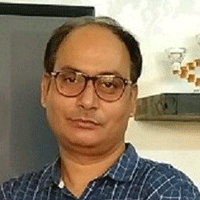 नरेश गोस्वामी
06 मई 2025
नरेश गोस्वामी
06 मई 2025
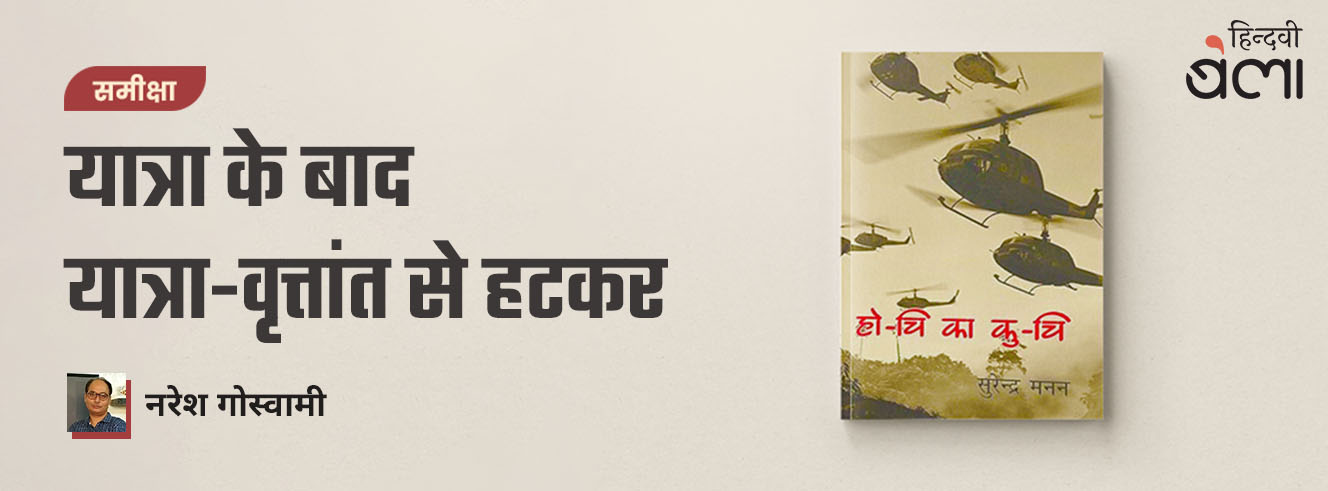
जैसे कुमार अंबुज फ़िल्मों पर लिखते हुए फ़िल्म की समीक्षा नहीं करते, बल्कि उसके दृश्यों, संकेतों, अर्थों और आशयों की तहों को खोलते हुए एक स्वतंत्र कृति की रचना कर देते हैं, वैसे ही डॉक्यूमेंट्री फ़िल्मों सृजक सुरेन्द्र मनन अपनी यात्राओं के अनुभवों को इतिहास और समकालीनता की पूर्वापर कड़ियों, सामयिक विश्लेषण तथा विधा की हदबंदियों का अतिक्रमण कर एक ऐसा समांतर पाठ तैयार करते हैं; जो केवल यात्रा का वृत्तांत न रहकर कुछ ऐसा बन जाता है, जिसे पढ़े जाने का क्षण में कोई एक नाम नहीं दिया जा सकता। यात्रा चलती रहती है, लेकिन उसका फ्रेम और भू-दृश्य बदल जाता है।
सुरेन्द्र मनन का यात्रा-वृत्तांत ‘हो-चि का कु-चि’ (संभावना प्रकाशन, संस्करण : 2022) यात्रा के दृश्यांकन के बजाय दृश्य के उस परावर्तन की किताब है, जिसमें देखने की क्रिया का प्रतिबिंब किसी भीतरी दीवार पर जाकर चमकता है।
मसलन, वियतनाम की यात्रा पर एकाग्र चार अध्यायों की पहली कड़ी में लेखक वियतनामी गुरिल्ला दस्तों द्वारा पहले फ़्रांसीसी और बाद में अमेरिकी सेनाओं के हमलों से बचाव के लिए बनाई गई एक भूमिगत सुरंग के अंदर दाख़िल होता है, जहाँ भीतर का दृश्य कुछ इस तरह खुलता है :
‘‘...और तभी अचानक मुझे अपनी साँसों की आवाज़ सुनाई दी। अँधेरी क़ब्र में एक ज़िंदा देह? मैं आँखें गड़ाए इस ज़िंदा देह को देखने लगा, जिसके नथुनों से निकलती हवा के कारण मिट्टी के कण अलसाये-से उठ-बैठ रहे थे। उस नीरवता में साँसों की आवाज़ ज़मीन से टकराती हुई सुरंग की दीवारों पर बिछल रही थी।"
इसके बाद जब लेखक सुरंग के अँधेरे से निकलकर बाहर आता है तो वह उस एकांत की नहीं, बल्कि वियतनाम की जनता के अपनी धरती से प्यार और जीवट की बात करता मिलता है :
‘‘जिस सुरंग से मैं बाहर निकला था, इस जंगल की ज़मीन के नीचे उससे जुड़ती एक दूसरी सुरंग थी। वह दूसरी सुरंग, तीसरी सुरंग में जा खुलती थी, जो चौथी सुरंग से जा मिलती थी, जहाँ से पाँचवीं सुरंग शुरू होती थी, जो छठी सुरंग तक जाकर ख़त्म होती थी... और इसी तरह ज़मीन के नीचे सैकड़ों सुरंगों का जाल बिछा हुआ था। धरती के ऊपर रबर के पेड़ों का घना जंगल, और धरती के नीचे इस सिरे से उस सिरे तक बलखाती आँतों की तरह फैला हुआ एक समूचा सुरंग-तंत्र! आश्चर्य यह कि सुरंगों का यह जाल सैंकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था। ...असल में यह एक समूची ऐसी दुनिया थी, जो धरती के गर्भ में बना और बसा ली गई थी और जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल भिन्न और अनोखी थी।’’ (पृष्ठ : 17)
मेरे ख़याल में, यह इन यात्रा-कथाओं का वह पहला क्षण है जब हम देखे हुए दृश्य को बाहरी यथार्थ की एक वृहत्तर संरचना में परावर्तित होते देखते हैं। एक तरह से देखें तो यात्राओं की यह किताब परावर्तन के ऐसे ही क्षणों की एक शृंखला है।
मिसाल के तौर पर, युद्ध की स्मृतियों और अवशेषों के संग्रहालय में रखी चीज़ों को देखते हुए लेखक ख़ुद को एक ऐसी दुनिया में पाता है ‘जहाँ कुछ भी ढकने-छिपाने या बताने की गुंजाइश न बचती थी। जब तक उस क्षेत्र में प्रवेश न करें, सब कुछ सामान्य, सहज, सुहावना था, लेकिन जैसे ही उसके भीतर क़दम रखें, यकायक सारा चैन, सुकून छिन जाता था। सारा शरीर मानो सवालों के तीखे नश्तरों से बिंध जाता; क्योंकि एक के बाद एक गिरते परदे ऐसे अविश्वसनीय, लेकिन वास्तविक चित्र आँखों के सामने उद्घाटित करते, जिन्हें देखते ही रूह काँप उठे। नरसंहार, रक्तपात, विध्वंस, समूल नष्ट कर देने का जो बेमिसाल जज़्बा उस दुनिया में ठाठें मारता था—उसे समझ पाने और ग्रहण कर पाने के लिए वाक़ई कड़े माद्दे की ज़रूरत थी।’’ (पृष्ठ : 68)
वियतनाम की जनता पर थोपी गई इस विभीषिका के पश्च-प्रभावों को देखने-समझने के लिए लेखक देहात में जाकर युद्ध में अपंग हुए लोगों से मिलता है और फिर युद्ध की उस त्रासदी का ब्योरा लिखता है, जिसका पूरा चेहरा युद्ध की समाप्ति के बाद उभरता है।
लेखक बताता है कि वियतनामी जनता और उसके गुरिल्ला संगठन—वियतकांग का ज़मीनी आधार ख़त्म करने के लिए अमेरिकी फ़ौजों ने ‘एजेंट ऑरेंज’ नामक एक ऐसे भयावह केमिकल का लंबे समय तक इस्तेमाल किया था, जो हरे-भरे जंगलों और फ़सलों को देखते-देखते राख में बदल देता था। इसका छिड़काव लगभग 66000 वर्गमील क्षेत्र पर किया गया, जिसके चलते पचास लाख एकड़ से ज़्यादा का जंगल ख़ाक हो गया और पाँच लाख एकड़ के रक़बे पर खड़ी फ़सलें तबाह हो गईं। साफ-स्वच्छ पानी के स्रोत ज़हरीले हो गए और आने वाले दशकों तक के लिए पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया। वियतनाम रेडक्रास के अनुसार ‘एजेंट ऑरेंज’ के असर से लगभग चालीस लाख लोग प्रभावित हुए और लगभग दस लाख लोग पूरी तरह अपंग हो गए। (पृष्ठ : 69)
चूँकि सुरेन्द्र मनन के लिए यह यात्रा सैर-सपाटा नहीं है, इसलिए युद्ध के विध्वंस के बाद उभरे नए वियतनाम को शहर के चौराहे से देखते हुए भी वे उसके त्रासद इतिहास को नहीं भूल पाते।
दृश्य के परावर्तन का एक ऐसा ही क्षण एथेंस के अपोलो मंदिर के उजाड़ में घटित होता है, जहाँ लेखक खुले आसमान के नीचे अकेला बैठा है :
‘’मंदिर के खंडहर सीपिया रंग की धूप में स्थिर खड़े थे। उनकी आड़ी-तिरछी छायाएँ मेरे अगल-बग़ल छिटकी थीं। पत्थर के स्तंभ, चबूतरे, टूटी मेहराबें... यह हाशिया पुरातन ग्रीक संस्कृति के प्रतीक-चिह्न के रूप में जैसे आसमान पर अंकित था। पूरा ढाँचा ऐसा आभास दे रहा था, जैसे किसी योद्धा के अंग-अंग काट दिए गए हों, लेकिन फिर भी अपराजित मुद्रा में वह अडिग खड़ा हो। उसी तरह अनश्वर जैसा कि ग्रीक और रोमन मिथकों में अपोलो का स्थान है। उसे प्रकाश, ज्ञान, संगीत और सच्चाई का देवता माना गया है; जिसके कारण ही इस संसार का कोई सत्व है। अपोलो का निवास इसी ओलिम्पस पहाड़ पर था। इस समय मैं उसी के निवास स्थान पर उपस्थित था। (पृष्ठ : 83)
दृश्य को देखते हुए उससे बाहर चले जाने का एक और क्षण लेखक की आर्मेनिया यात्रा में आता है। अपनी ज्ञात स्मृतियों में अनवरत बहिष्कार, अपमान और जातीय संहार की अमानवीय परिस्थितियों से लड़कर ज़िंदा रही आर्मीनी जनता के देश में एक फ़िल्म समारोह में शिरकत करने गए सुरेन्द्र मनन मौक़ा मिलते ही तासि्तसर नकाबर्ड कॉम्प्लेक्स (आर्मीनी जाति संहार स्मारक) पहुँच जाते हैं। और हम देखते हैं कि संहार की स्मृतियों ने उन्हें कैसे संज्ञा-शून्य कर देती हैं :
‘‘मैं एक अजीबोग़रीब अनुभूति की गिरफ़्त में था। स्मारक की हदबंदी में पहुँचते ही न तो मन में किसी जिज्ञासा का भाव रहा, न ही कोई उतावली बची थी। जैसे-जैसे मैं क़दम आगे बढ़ा रहा था, एक ठंडापन भीतर उतरता जा रहा था। जाने क्या वजह थी जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी। क्या मैं स्मारक के रू-ब-रू होने से बच रहा था? कहीं मुझे यह लग रहा था कि जब तक मैं बाहर हूँ; फिर भी अछूता हूँ, लेकिन भीतर पहुँचने पर पलायन का कोई रास्ता न बचेगा? मेरे पैर निरुद्देश्य थे। वे इधर-उधर कुछ भटके, फिर जैसे छिपने की कोई जगह न पाकर स्थिर हो गए।’’ (पृष्ठ : 100)
इस सिलसिले में अगला क्षण नाथूला दर्रे का है, जिसे 1962 के भारत-चीन युद्ध के चालीस बरसों के बाद 2003 में दुबारा व्यापार के लिए खोला गया था। दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार और संपर्क की बहाली के बाद लेखक 2006 में यहाँ एक वृत्तचित्र की शूटिंग के लिए पहुँचा था। कड़ाके की सर्दी, फ़ौजी निगरानी, निर्जनता और सन्नाटे के बीच नाथूला की ओर बढ़ते हुए अचानक एक ऐसी जगह आई, जहाँ लेखक को लगा कि जैसे वह किसी रहस्यलोक में पहुँच गया है :
‘‘गाड़ी से उतर, उस लोक के सन्मुख खड़ा मैं पलक झपकाना तक भूल गया। साँस रोके, बस उस गहरे नीले रंग की अंडाकार झील पर टकटकी लगाए खड़ा रहा जो पहाड़ों के बीच शांत लेटी थी। मानो नीले रंग का कोई बड़ा-सा नगीना पहाड़ों की झोली में आ गिरा हो! गिर कर वहीं अटक गया हो, स्थिर हो गया हो। यह छंगु झील थी। झील के पास स्तब्ध, स्तंभित-सी अवस्था में खड़े मुझे लगा कि मेरा सब कुछ पीछे छूट गया है। वह सब परत-परत अलग होकर विलीन हो रहा है, जिसमें मैं अभी तक लिपटा-लिथड़ा हुआ था। उस दुनिया से मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, जिसका अभी तक अभिन्न हिस्सा बना साँस ले रहा था। (पृष्ठ : 118)
यात्रा के इस सम्मोहक और अयाचित क्षण के बाद वह क्षण आता है, जहाँ दोनों देशों की सीमा-रेखा पर लेखक अपना एक पैर भी नहीं रख सकता। यह नाथूला दर्रे की चेकपोस्ट का दृश्य था। भारतीय सीमा पर ट्रकों की आवाजाही और गतिविधियों को फ़िल्माने के बाद लेखक चीनी अधिकृत क्षेत्र की सड़कों और पर्वत शृंखला का वाइड शॉट लेना चाहता था। इसके लिए उसे केवल दो क़दम आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। लेकिन, लेखक ने जैसे ही ‘नो मैंस लैंड’ के बाहर क़दम उठाया तो सीमा के दूसरी तरफ़, फाटक के दाएँ-बाएँ मुस्तैद खड़े चीनी-सैनिक लपक कर सामने आ गए और लेखक का उठा हुआ पैर वहीं हवा में अटका रह गया।
यह घटना लेखक को अन्यमनस्क कर देती है। वह लिखता है कि उसे ज़मीन के बँटवारे और ऐसे नियम-क़ानूनों के बारे में पता था :
‘‘लेकिन इस तथ्य का इतनी गहराई और विकटता से अहसास मुझे अभी हुआ था—अधर में अटके हुए उस एक क़दम के कारण। वह उस धरती पर नहीं रखा जा सकता था, जो एक क़दम भर के दायरे में ही तो थी। बिल्कुल वैसी ही तो थी, जैसी इस तरफ़ थी। लेकिन उसे विभाजित करके शस्त्रों से लैस दोनों तरफ़ खड़े सैनिक दावा कर रहे थे कि नहीं, वह अलग क़िस्म की है। मैं उसे उस तरह से नहीं देख सकता, जैसे कि इस तरफ़ की धरती को देख सकता हूँ और कि मेरी पहुँच से वह बाहर है। (पृष्ठ : 127)
यात्राओं के इस कोलाज में बांस्का बिस्त्रिका (स्लोवाकिया) का पड़ाव अपनी माहौल-साज़ी के लिए अलग से दमकता है। लेखक इस शहर में आयोजित एक फ़िल्म समारोह में बतौर अतिथि आया है। आयोजन-समिति की प्रमुख सदस्या एंड्रिया लेखक को उसके होटल की बाल्कनी से एक म्युजियम की ओर संकेत करते हुए बताती है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फ़ाशिस्ट जर्मनी का इसी जगह से प्रतिरोध किया गया था। एंड्रिया लेखक से आग्रह करती है कि वह उस जगह ज़रूर जाए, लेकिन इस ताक़ीद के साथ कि ‘आप मेरे शहर और देश को किसी म्युजियम की तरह नहीं देखेंगे’ क्योंकि ‘ऐसा करेंगे तो कुछ भी नहीं जान पाएँगे।’ इस पर जब लेखक उससे पूछता है कि इसके लिए उसे क्या करना होगा तो एंड्रिया खिलखिलाते हुए कहती है : आपको अपनी अजनबियत की दीवार को तोड़ना पड़ेगा... ख़ुद को पहले यह बताना पड़ेगा कि आप मेरे देश, मेरे शहर के वासी हैं। इस जगह का ही अंग हैं—कहीं बाहर से नहीं आए।
बाद में, लेखक एंड्रिया की इस दोस्ताना सलाह पर किसी दूसरी जगह और चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अमल करता है। समारोह के कार्यक्रमों से फ़ारिग़ होकर एक शाम वह शहर के भीतरी इलाक़ों से लौटकर एक रेस्त्राँ पहुँचता है। लेकिन, वह जैसे ही खाना शुरू करता है तो बारिश पड़ने लगती है। उसके ज़ेहन में अचानक एक ख़याल आता है। वह नीचे से जिन खुली और चौड़ी सीढ़ियों से चढ़कर रेस्त्राँ तक पहुँचा था, उनसे वापस उतरने लगता है। चारों तरफ़ अँधेरा है। बारिश तेज़ हो गई है। रेस्त्राँ के काउंटर पर बैठी लड़की उसे पुकार कर रुकने के लिए कहती है। लेकिन लेखक सीढ़ियाँ टटोलते हुए लगातार निचाई की ओर बढ़ता चला जाता है :
‘‘मैं पानी की लहरों पर डगमगाती हुई किसी नाव की तरह था जो हवा और पानी के थपेड़े खाती किनारा ढूँढ़ रही थी। मैं स्लोवाकिया के अंधकारपूर्ण आसमान के नीचे था, मैं बांस्का की बारिश में भीग रहा था, मैं बिस्त्रिका के भूगोल को टटोल रहा था। मैं एक ऐसे लगातार झरते घटाटोप में घिरा था जहाँ न मुझे कोई देख सकता था, न मेरी पहचान के दायरे में ही कोई था। उस देश, उस काल, उस स्थिति से उपजे विराट अंधकारमय शून्य में, मैं किसी बुलबुले की तरह तैर रहा था।... अब इस ज़मीन आसमान में मैं उतना ही अंतरंग और आत्मीय जितना कि यहाँ का कोई प्राणी। (पृष्ठ : 145-46)
इन यात्राओं का एक सफ़हा मौजूदा हिमाचल प्रदेश के एक नामालूम गाँव दिग्शाई से भी वाबस्ता है। दिग्शाई यानी दाग़े शाही—यानी मुग़ल राज्य के ख़िलाफ़ बग़ावत करने वाले लोगों के माथे पर दाग़ी जाने वाली शाही मुहर। ऐसे लोगों को दाग़ लगाकर हिमाचल के इस चारों ओर एक के बाद कई पर्वत-शृंखलाओं से घिरे इलाक़े में छोड़ दिया जाता था, जहाँ से वे कभी वापस नहीं लौट पाते थे। ज़िंदा बचे लोगों का धीरे-धीरे यहाँ एक गाँव बस गया और समय के साथ दाग़े शाही घिसते-घिसते दिग्शाई हो गया।
बाद में, उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान जब अँग्रेज़ पंजाब और पश्चिमोत्तर क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने इसी जगह एक आधुनिक जेल का निर्माण किया। किताब का यह अध्याय अँग्रेजों द्वारा निर्मित इसी जेल के बारे में है। जनजीवन की हलचलों से दूर एक अल्पज्ञात पहाड़ी गाँव में वक़्त के साथ टूटती-ढहती इस इमारत की एक कोठरी में खड़ा लेखक सत्ता-तंत्र और दंड की व्यवस्था पर सोच रहा है :
‘‘कोठरी के भीतर लकड़ी के फ़र्श पर क़दम रखते ही एक आवाज़ गूँजती है। आवाज़ आस-पास सिमटी दीवारों के बीच उमड़ती-घुमड़ती हुई ऊँची छत की तरफ़ उठती है। छत से टकरा कर वापिस लौटती है तो उसकी गूँज देर तक सनसनाती रहती है। दीवारें। ठंडी, सपाट दीवारें। आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ सिर्फ़ दीवारें। इतनी क़रीब कि दो क़दम आगे बढ़ें तो रोक लें, दो क़दम पीछे हटें तो रोक लें। आँखों के लिए देखने को दीवारें। हाथों के स्पर्श के लिए दीवारें। बात करने के लिए दीवारें। बात सुनने के लिए कान सटाने को दीवारें। सिर पटकने को दीवारें। पस्त होकर गिर पड़ने के बाद सहारा देने को दीवारें। अंग-संग हर पल, हर घड़ी, हर समय सिर्फ़ दीवारें।’’ (पृष्ठ : 148)
यात्राओं का यह सिलसिला थाइलैंड पर जाकर रुकता है। यात्रा के इस आख़िरी पड़ाव से लेखक थाइलैंड के इतिहास पर नज़र डालते हुए उसके वर्तमान तक आता है। वह रोज़मर्रा के जीवन और स्थलों—सड़कों, समुद्र तटों, शॉपिंग मॉल्स और फ़ुटपाथों के बिंबों से उस लंबी प्रक्रिया की निशानदेही करता है जिससे गुज़रते हुए सात-आठ दशक पहले का धान की खेती का उर्वर देहात और एक धर्मनिष्ठ समुदाय—बैंकाक, उपभोग और दैहिक कामनाओं की मंडी बन जाता है। यह एक तरह से बैंकाक के बाज़ार में रूपांतरण की आँखों देखी रिपोर्ट है। अब लगभग हर कोई यह बात जानता है कि बैंकाक का पत्थया समुद्र-तट भारत के अमीर लंपटों का भी अड्डा बन गया है।
पत्थया को बाज़ार और दैहिक कामनाओं के बीच रखकर सुरेन्द्र मनन उसके कई संस्तरों पर एक-साथ नज़र डालते हैं :
‘‘पत्थया थाईलैंड का दूसरा चेहरा है... पत्थया, जो कभी मछुआरों का छोटा-सा गाँव था, आज थाईलैंड का प्रमुख पर्यटन-स्थल है... पत्थया एक ललकार है। सर्वशक्तिमान राजा हो या पूजनीय बौद्ध भिक्षु, मंदिरों में प्रार्थनारत लोग हों या दिव्य चुप्पी का साम्राज्य, पवित्र प्राचीन वाट हों या रामकीयन की प्रस्तुतियाँ, या फिर एक महान् सांस्कृतिक विरासत हो—पत्थया सबको ठेंगे पर रखता है!... पत्थया में न स्वयंसिद्ध चुप्पी है, न प्रार्थना में जुड़े हाथ हैं, न कुलीनता और शालीनता है। शाम उतरते ही यहाँ रंग-बिरंगी चुस्त, भड़कीली पोशाकों में लड़कियाँ अनार के दानों की तरह सड़कों पर बिखर जाती हैं, जिन्हें कोई भी दाम चुकाकर मुट्ठी में भर सकता है। दलाल इशारों से या गुपचुप नहीं, खुलेआम बोलियाँ लगाते हैं। अधेड़, बूढ़े गोरे सैलानी बग़ल में सोलह-सत्रह बरस की थाई लड़की लिए समुद्र किनारे अठखेलियाँ करते दिखायी देते हैं।’’ (पृष्ठ : 190)
ख़ैर, अब जब हम इस यात्रा के आख़िरी मक़ाम पर पहुँच गए हैं तो दिमाग़ में रह-रहकर यह ख़याल उठ रहा है : यात्रा का यह वृत्तांत आम, औसत या मुख्यधारा के वृत्तांतों से किस मायने में अलग है?
और इस पर सोचते हुए मुझे लग रहा है कि असल में, सुरेन्द्र मनन की यह किताब कहीं पहुँचने और लौट आने के बीच खींची गई तस्वीरों की एलबम या नामों की फ़ेहरिस्त नहीं है। दरअस्ल, वह सैर-सपाटे और पर्यटन की मध्यवर्गीय-उपभोक्तावादी छवि को प्रश्नांकित करती है और देखे हुए को रनिंग कमेंट्री में अपघटित करने के आसान फ़ार्मूले का प्रतिकार करती है। शायद इन्हीं दो कामों में उसकी यह उपलब्धि निहित है कि वह यात्रा को कला, चिंतन, विमर्श और अज्ञात के साक्षात्कार के क्षण में अंतरित कर देती है।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
12 जून 2025
‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही’
‘बॉर्डर 2’ का विचार सुनते ही जो सबसे पहला दृश्य मन में कौंधा, वह बालकनी में खड़े होकर पिता का कहना था—‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही।’ इस वाक्य में सिर्फ़ एक अभिनेता का अवसान नहीं था, एक पूरे युग क
29 जून 2025
‘बिंदुघाटी’ पढ़ते तो पूछते न फिरते : कौन, क्यों, कहाँ?
• उस लड़की की छवि हमेशा के लिए स्टीफ़न की आत्मा में बस गई, और फिर उस आनंद में डूबा हुआ पवित्र मौन किसी भी शब्द से नहीं टूटा... आप सोच रहे होंगे कि यहाँ किसी आशिक़ की किसी माशूक़ के लिए मक़बूलियत की बा
14 जून 2025
बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल!
‘बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल’—यह नब्बे के दशक में किसी पल्प साहित्य के बेस्टसेलर का शीर्षक हो सकता था। रेलवे स्टेशन के बुक स्टाल्स से लेकर ‘सरस सलिल’ के कॉलमों में इसकी धूम मची होती। इसका प्रीक्वल और सीक्वल
10 जून 2025
‘जब सोशल मीडिया नहीं था, हिंदी कविता अधिक ब्राह्मण थी’
वर्ष 2018 में ‘सदानीरा’ पर आपकी कविता-पंक्ति पढ़ी थी—‘यह कवियों के काम पर लौटने का समय है’। इस बीच आप फ़्रांस से लौटकर आ गए। इस लौटने में काम पर कितना लौटे आप? 2018 में जब यह कविता-पंक्ति संभव हुई
20 जून 2025
8/4 बैंक रोड, इलाहाबाद : फ़िराक़-परस्तों का तीर्थ
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एम.ए. में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी मेरे मित्र बन गए। मैं उनसे उम्र में छोटा था, लेकिन काव्य हमारे मध्य की सारी सीमाओं पर हावी था। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। उनका नाम वीरेंद्र