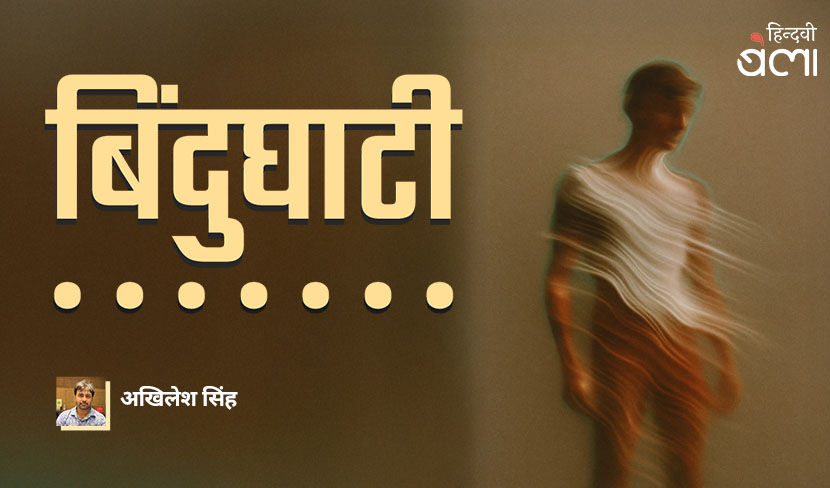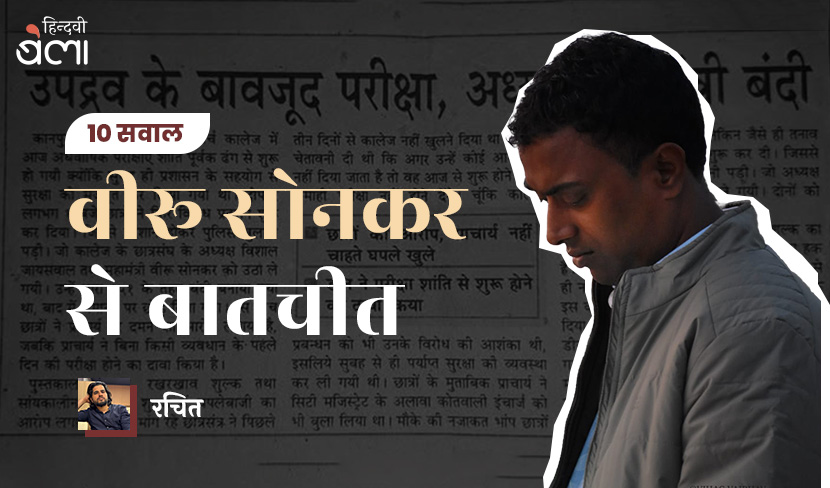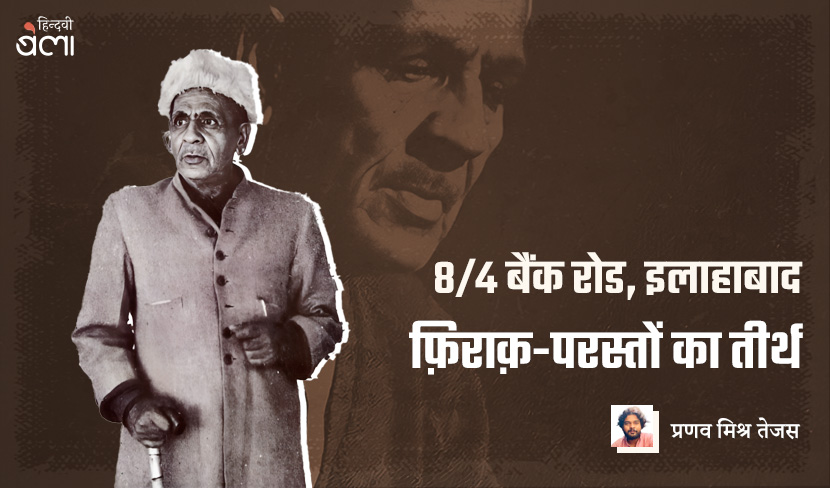पूर्वांचल के बंकहों की कथा
 श्वेता त्रिपाठी
17 जून 2025
श्वेता त्रिपाठी
17 जून 2025

कहते हैं इवोल्यूशन के क्रम में, हमारे पूर्वज सेपियंस ने अफ़्रीका से पदयात्रा शुरू की थी और क्रमशः फैलते गए—अरब, तुर्की, बाल्कन, काकेशस, एशिया माइनर, भारत, चीन; और एक दिन हर उस ज़मीन पर उनकी चरण पादुकाएँ पाई गईं जो खारे पानी से लबालब भरे कटोरे के ऊपर तैरती थी। हमने उन आदिम लोगों को नहीं देखा था, लेकिन अब एक अदद नौकरी के लिए झोरा-झंटा उठाए लोगों को गाँव से क़स्बे, क़स्बे से शहर और देश से विदेश भागते हुए देखकर लगता है कि ऐसे ही फैले होंगे लोग। पहले लोग कहीं नहीं जाते थे, फिर अपने सबसे क़रीबी शहर जाने लगे, उससे भी काम न चला तो कुछ लोग कोइलरी में काम करने झरिया गए, कोइलरी की कमाई से भी न बना तो लोग कलकत्ते की ओर भागे और एक दिन सरहद की कंटीली दीवार फाँदकर रंगून भी पहुँचे, लेकिन रंगून भी कितने दिन सँभाल सकता था। रंगून ने जवाब दे दिया तो नया ठौर तलाशा गया—बंका।
बंका, लंका का भाई नहीं था। वह रंगून का पट्टीदार था। बंका का शुभ नाम बैंकाक है। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर के सेपियंस उसे प्यार से बंका बुलाते हैं। यह उसका पुकार नाम है। ये लोग बैंकाक नहीं जाते—बंका जाते हैं, बंका में रहते हैं और वहीं से वापस भी आते हैं। गाँव के लोग इन्हें बंकहा कहते हैं। वैसे ही जैसे राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल शिवपालगंज के निवासियों को गंजहा कहते हैं। यहाँ सवाल यह भी है कि कोई सूरत जाने वाले को सूरतिहा, बैंगलोर जाने वाले को बैंगलोरहा और रंगून जाने वाले को रंगूनहा नहीं कहता तो बंका जाने वाले को बंकहा क्यों कहा गया? इसका जवाब यह है कि एक बार बैंगलोर में कमाने गया आदमी, बंबई में भी काम कर सकता है; सूरत गया हुआ आदमी लुधियाना भी चला जा सकता है, लेकिन जो एक बार बंका में उतर गया वह हर बार बंका ही जाएगा। बंका उसका स्थायी पता बन जाता है। जो आदमी, नागरिक भारत का होता है लेकिन निवासी बंका का, वही बंकहा होता है। कुछ लोग किसी थाई महिला से ब्याह करके बंका की नागरिकता भी ले लेते थे, वे भी बंकहा ही कहे जाते थे और बंका में इस तरह की शादियों की एक स्थापित व्यवस्था भी थी।
कुछेक अपवादों के साथ, बंकहा वो बाभन-ठाकुर थे जो कल्याण सिंह के पहले और उनके राज में हुई नकलविहीन परीक्षा के चलते दसवीं और बारहवीं में कम-से-कम दो बार फ़ेल हुए और तीसरी बार बड़ी कोशिशों और मन्नतों से थर्ड डिवीजन लाने में कामयाब हो पाए। जिन्हें नब्बे के दशक में कोई कामचलाऊ नौकरी भी न मिली और सबसे ज़रूरी बात कि वे किसी वर्तमान या भूतपूर्व बंकहे को जानते थे। इस प्रकार के वर्तमान और भूतपूर्व बंकहों की प्रवृत्ति वैसी ही थी—जैसी आजकल के ‘दिल्ली आजा’ या ‘बेंगलुरु आजा’ बोलने वाले कॉरपोरेट मज़दूरों की है। बंकहे भी ‘बंका चलो’ के नारे पर थाइलैंड में ‘आज़ाद हिन्द फ़ौज’ बनाना चाहते थे।
पुराने बंकहे नए रंगरूटों को बंका में ‘उतारते’ थे, लेकिन नाव से नहीं, हवाई जहाज़ से। ये लोग माडर्न डेज़ केवट थे और केवट की ही तरह कई बार कुछ ‘उतराई’ भी लेते थे। एक चचा थे जिन्हें गाँव के ही एक दूसरे चचा ने एक बार बंका उतारा था और बदले में कुछ पुश्तैनी ज़मीन ले ली थी। अफ़सरी लायक़ न बचे बाभन-ठाकुरों के लिए बंका विकल्प नहीं था, अनिवार्यता थी। अहीरों और कुर्मियों के लड़के गए फ़ौज में, कोइरियों ने उगायी हरियाली, बनियों के लड़कों ने सँभालीं गल्ले-गोदाम की चाभियाँ। ठाकुरों के लड़के, जिनके अपने खेत भी बेलदारों ने बंटाई पर आबाद किए थे, वे देश में ‘कहीं भी’ जा तो सकते थे, लेकिन ‘कुछ भी’ नहीं कर सकते थे। विदेश, बंका उनकी इस झिझक से परे था। वहाँ कोई बेलदार, बनिया, कुर्मी नहीं देख रहा था; बाबू साहब और पंडी जी को, फौराट की गलियों में फ़ेरी लगाकर सामान बेचते हुए। बंका प्रतिष्ठा की हानि के भय से मुक्त करता था। लेकिन साथ ही एक दूसरे भय को जन्म भी देता था—पकड़े जाने का भय। दरअस्ल बहुत से बंकहे बंका में लीगली नहीं रहे होते थे। वो बहुधा एक वाक्यांश इस्तेमाल करते थे—बीसा खाट हो जाना। यानी वीज़ा की अवधि ख़त्म हो जाना। कई बंकहे वीज़ा ख़त्म होने के बाद ग़ैर-कानूनी रूप से कई साल ओवरस्टे करते थे। कुछ लोग छह महीने के वीज़ा पर गए और छह बरस बाद लौटे। कई बार पुलिस पकड़ लेती। ये कुछ ले-देकर बच निकलते और आख़िरकार जब देश लौटना चाहते तो किसी थाने में सरेंडर कर देते थे। फिर वहाँ की सरकार इन्हें अपने देश भेज देती थी। इन सब के बीच कितनी बार पकड़े और छोड़े गए नहीं मालूम। बंकहों ने बैंकाक पुलिस का गहन विश्लेषण किया था और इस नतीजे पर पहुँचे थे कि पुलिस की जात सब जगह एक जैसी ही है—सब घूसख़ोर हैं, पैसे देने पर छोड़ देते हैं। बंकहे पकड़ाते-छूटते रहे और परदेस में एक-दूसरे को सहारा भी देते रहे। जिन दो पटीदारों के बीच ज़मीनी विवाद चल रहा था, उनके लड़के भी बंका में एक ही कुकर में पकाया मीट-भात खाते रहे और कँधे पर एक पुरानी डोलची टांग कर बेचते रहे कभी भूंजा, कभी चाय, कभी साबुन, कभी घड़ी और कभी मसहरी।
वैसे बंका का सबसे मज़बूत फ़ैक्टर था उसकी करेंसी—बाट। मैंने लोगों को कहते सुना था कि “बंका क पइसा इहां से बड़वार है। ओहां क एक रुपया एहां डेढ़ रुपया से बेसी हो जाला।” लेकिन बचपन में इतना ही अंदाज़ा लगा पाई थी कि साइज़ में बड़ा होता होगा। बाद में करेंसी का खेल समझा तो जान पाई कि लोग कलकत्ते से रंगून और रंगून से बंका क्यों गए थे और जब गए तो बरसों तक क्यों नहीं लौटे—क्योंकि वहाँ का पैसा बड़ा था। बड़ा पैसा ही महत्वपूर्ण था। प्रतिष्ठा तो उस पैसे की पिछलग्गू थी। उसे तो आना ही था।
छह-छह, सात-सात साल बाद बंकहे जब अपने गाँव लौटे तो उनके बच्चों ने भी उन्हें नहीं पहचाना। तीन साल की बच्ची बार-बार अपने पिता की ओर दिखाते हुए माँ से कहती रही कि यह घर में जो आदमी आया है वह तुम्हारे कमरे में क्यों बैठता है? कौन है? यह तो मैंने ख़ुद देखा था। हालाँकि पत्नियाँ कभी अपने पतियों की शक्ल नहीं भूलीं, आवाज़ शायद धुँधली पड़ती रही होगी, मुझे ठीक-ठीक अंदाज़ा नहीं है।
बंकहों की पत्नियों ने कई बार उर्मिला का-सा वनवास काटा। साल में बमुश्किल एक या दो बार आने वाली चिट्ठियों के सहारे बिताया यौवन। उन्हें ‘बंकहा की मेहरारू’ कहा गया— बंका से आई समस्त संपदा की कोषाधिकारिणी। गले में कम-से-कम तीन भर की सीकड़ और, भड़कीले लॉकिट वाला मंगलसूत्र, दुतल्ला झुमके से भार से लगभग लटकते हुए कान और उँगलियों में भौड़ी-ड़कीली, बेडौल डिजाइन वाली अंगूठी, जिसे लोग बंका की अंगूठी कहते थे और ऐसी नज़र से देखते थे जिसमें प्रशंसा, बखान के साथ लालच का पुट भी था। ये सब अभिप्राय बंकहों की पत्नियों का शृंगार थे। ऐसी ही थीं बंकहों की पत्नियाँ, रूप से लक्ष्मी, भाग्य से उर्मिला। उस दौर में, इन औरतों ने तीज-चौथ कैसे काटी होगी! कैसे मनाये होंगे पर्व! सोचती हूँ कि अट्ठारह-बीस बरस की कुलांचे भरती हुई किशोरियों को कैसा लगता होगा; जब उनका ब्याह जब किसी ऐसे लड़के से तय हुआ होगा, जिसके बारे में यह पूर्व निर्धारित था कि वह कई-कई बरस तक दूर बिदेस में रहेगा। बहुत बरस बाद, कुछ महीनों के लिए ही साथ रह सकेगा। कैसा होगा उन नवोढ़ाओं का जीवन जिनके भाग्य में भरपूर शृंगार था किंतु साहचर्य नहीं। उन्होंने अपने पति के किसी थाई लड़की से ब्याह की घटना पर कैसी प्रतिक्रिया दी होगी? वे सखियों को अपने गहने-गदेले गिना कर ख़ूब इतरा सकती थीं, लेकिन बिदेसिया और जंतसार के गीतों पर रोना भी उन्हीं के हिस्से में आया। उन्हीं नववधुओं ने जना होगा बिदेसिया का यह गीत—हंसि हंसि पनवा खियवले बेइमनवा, कि अपना बसे रे परदेस। कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाइ गइले, मारे थे करेजवा में ठेस।
कितने कैरेट का सोना, कितने भर की सीकड़ और कौन-सा हार-हुमेल उनकी बरसों की वंचितता को तोप सकता था!
बंकहे केवल सोना ही नहीं लाए। वे साथ लाए लाल-नीली और बीच में कहीं-कहीं सफेद चारखाने की लुंगी, फूलों के प्रिंट वाली आधी बाँह की शर्ट, कप की छाप वाली नारंगी रंग की बाम की डिब्बी, बंकहवा सेंट और टॉर्च, चटख रंगों की पोलो टी-शर्ट, बैगी जीन्स, मैक्सी, लौंग का तेल और सपहवा पाउडर भी, जिसके सफ़ेद रंग के टिन के डिब्बे पर छपा होता था हरे रंग का साँप और लिखा होता था स्नेक ब्रांड। गाँव में सब इसे सपहवा ही कहते थे। मई-जून की गर्मी जब पीठ पर अम्हौरी (घमौरी) के लाल चितकबरे निशान बना देती थी और सारे देसी पाउडर बेअसर हो जाते थे, तब कोई माँगता था सपहवा। सपहवा अपने भयंकर ठंडे फ़ार्मुले से राहत पहुँचाता था। सपहवा इतना कारगर था कि लोग इस बात को नज़रअंदाज़ कर देते थे कि वह लगाते वक़्त थोड़ा छरछराता भी था।
इसके साथ ही अनजाने में बंकहों के लगेज के साथ ही चिपककर आई सियामी। थाइलैंड यानी सियाम की भाषा। बंका की भाषा। बंकहे गाँव आकर अपनी सियामी फ्लांट करते और किसी बच्चे को सिखा रहे होते—‘निंग, सांग, साम, सी, हां’ मतलब एक, दो, तीन, चार, पाँच। ‘गिन खाओ यांग’—क्या तुमने खाना खाया। ‘मइ तोंग फूत माक’—ज़्यादा मत बोलो। ‘सावाद्दी खाप’—नमस्ते। बचपन में इतना सीखकर मुझे लगता था कि मैं भी बंका जाने लायक़ हो गई हूँ।
बंकहों का लाया हुआ सामान उनके वस्त्र-विन्यास का अहम हिस्सा भी था। अगर गाँव में एक मोटी चेन और कम से कम छह अँगूठियाँ पहने कोई आदमी, सफ़ेद बाँहदार बंडी पहनकर, चारख़ाने की लुंगी को ठेहुने तक खुंटिया कर, गद्दे लगी चारपाई पर इतना पाउडर लपेट कर बैठा हुआ दिखे कि नागाओं के शरीर पर लिपटी भस्म का ध्यान हो आए तो समझना वह पुराना बंकहा है। नया बंकहा बैगी जीन्स और पोलो टी-शर्ट पहनता है, हालाँकि पाउडर और अंगूठी का मोह वह भी नहीं छोड़ पाया है। इसके साथ ही अच्छा कमाने वाला बंकहा बुलेट ज़रूर रखता था। जैसे यह उसके बंकहा होने का अशोक स्तंभ था।
बंकहे गोरखपुर, लखनऊ, कलकत्ता नहीं उतरते थे—इंडिया उतरते थे। मामला अब ज़िला जवार के बस स्टैंडों से आगे निकलकर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुँच गया था। जिस गाँव में कायदे से दुपहिया और चारपहिया भी मयस्सर न थीं, उस गांव में बंकहे हवाई यात्रा वृत्तांत सुनाते हुए यह स्वघोषित वैज्ञानिक तथ्य भी बताते थे कि बादल दरअस्ल रुई के फाहे हैं। जहाज़ इन रुई के फाहों को चीरते हुए आसमान में अपना रास्ता तय करता है। यह तथ्य सुनने तक मैंने अपनी किताबों में बादलों के बनने का विज्ञान समझ लिया था लेकिन एक तथ्य और था कि बंकहों ने विज्ञान को कभी सीरियस नहीं लिया था, भूगोल को भी नहीं। उनके लिए विश्व में दो महाद्वीप थे—बंका और इंडिया। वे भारत या हिंदुस्तान नहीं कहते थे। अपने गाँव-ज़िले का नाम भी नहीं लेते थे। उनके लिए सबकुछ इंडिया था। जैसे उनके लिए ही संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत, का कथन गढ़ा गया था। वे इंडिया में उतरे लड़कों का विवाह कराने और लड़कियों का विवाह ढूँढ़ने के लिए। लोग बंकहों की लड़कियों को ब्याह कर लाना चाहते थे क्योंकि वे केवल लड़कियाँ नहीं थीं, मोटे दहेज की गारंटी भी थीं। कई बार विवाह ढूँढ़ने के लिए आना नहीं पड़ता था। विवाह बंका में ही तय हो जाया करते थे। एक बंकहे का दूसरे बंकहे से रोटी का रिश्ता तो था ही, बेटी का रिश्ता भी होने लगा मानो बंकहा बाभनों की कोई उप जाति हो।
यही बंकहे इंडिया से बंका जाने के ठीक एक दिन पहले पता नहीं कौन-सी और कितनी प्राचीन परंपरा के तहत सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे। इस कथा का विजय (बुलावा) ही बंकहों के वापस जाने की मुनादी था और इस बात की भी कि अब उनकी कमाई धनराशि ख़त्म हो चुकी है और सपहवा पाउडर की खेप भी। अब फिर से बनवाना होगा—एक नए नाम का पासपोर्ट, फिर से लगवाना होगा नया टूरिस्ट या स्टूडेंट वीज़ा। बंका में उतरकर फिर टाँगनी होगी कंधे पर डोल्ची और फिर बेचना होगा भूंजा, चाय, साबुन, घड़ी या मसहरी, क्योंकि बंका का पैसा इंडिया से बड़ा है, इंडिया की ग़रीबी उससे बड़ी है और सबसे बड़ा है पूर्वांचल के इन बंकहों का जीवट।
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
12 जून 2025
‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही’
‘बॉर्डर 2’ का विचार सुनते ही जो सबसे पहला दृश्य मन में कौंधा, वह बालकनी में खड़े होकर पिता का कहना था—‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही।’ इस वाक्य में सिर्फ़ एक अभिनेता का अवसान नहीं था, एक पूरे युग क
29 जून 2025
‘बिंदुघाटी’ पढ़ते तो पूछते न फिरते : कौन, क्यों, कहाँ?
• उस लड़की की छवि हमेशा के लिए स्टीफ़न की आत्मा में बस गई, और फिर उस आनंद में डूबा हुआ पवित्र मौन किसी भी शब्द से नहीं टूटा... आप सोच रहे होंगे कि यहाँ किसी आशिक़ की किसी माशूक़ के लिए मक़बूलियत की बा
14 जून 2025
बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल!
‘बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल’—यह नब्बे के दशक में किसी पल्प साहित्य के बेस्टसेलर का शीर्षक हो सकता था। रेलवे स्टेशन के बुक स्टाल्स से लेकर ‘सरस सलिल’ के कॉलमों में इसकी धूम मची होती। इसका प्रीक्वल और सीक्वल
10 जून 2025
‘जब सोशल मीडिया नहीं था, हिंदी कविता अधिक ब्राह्मण थी’
वर्ष 2018 में ‘सदानीरा’ पर आपकी कविता-पंक्ति पढ़ी थी—‘यह कवियों के काम पर लौटने का समय है’। इस बीच आप फ़्रांस से लौटकर आ गए। इस लौटने में काम पर कितना लौटे आप? 2018 में जब यह कविता-पंक्ति संभव हुई
20 जून 2025
8/4 बैंक रोड, इलाहाबाद : फ़िराक़-परस्तों का तीर्थ
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एम.ए. में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी मेरे मित्र बन गए। मैं उनसे उम्र में छोटा था, लेकिन काव्य हमारे मध्य की सारी सीमाओं पर हावी था। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। उनका नाम वीरेंद्र