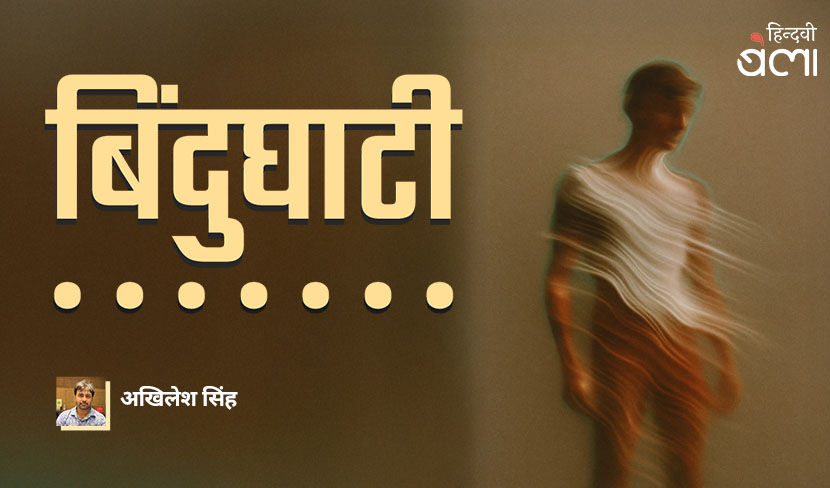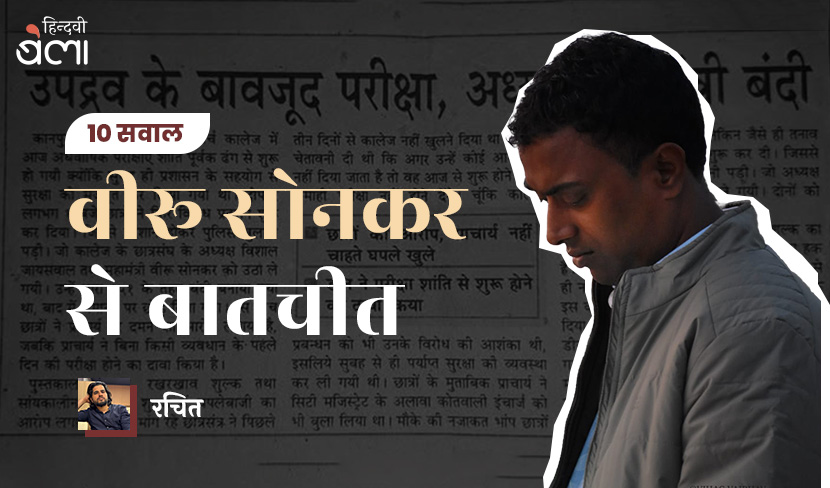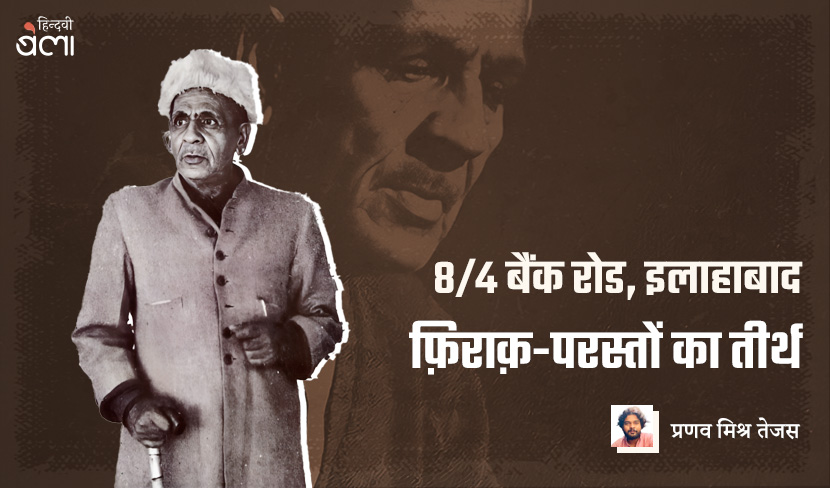कृष्ण कुमार : एक शालीन और साफ़ आवाज़
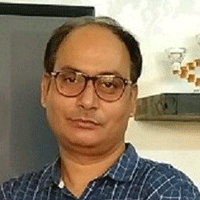 नरेश गोस्वामी
22 जुलाई 2025
नरेश गोस्वामी
22 जुलाई 2025
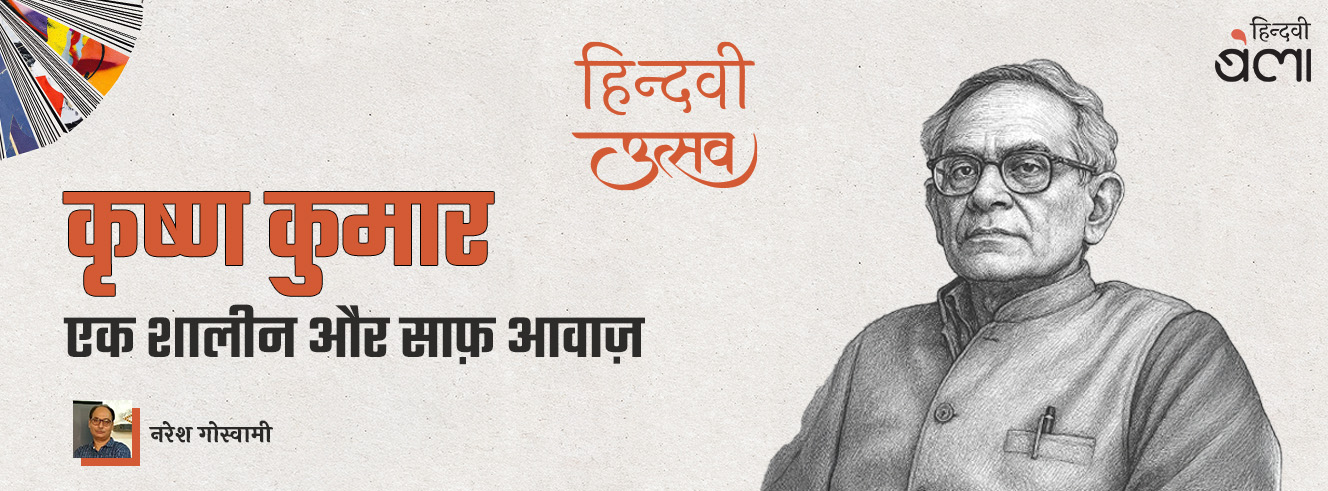
शिक्षाविद् कृष्ण कुमार के बारे में न्यूनतम कहना भी एक मुश्किल काम है क्योंकि ‘प्रसिद्ध’ या ‘लब्ध-प्रतिष्ठ’ जैसे विशेषणों से न उनके कृतित्व की महत्ता का अंदाज़ा होता है, न उनके काम की बहुआयामिता का आभास मिलता है। यह शायद इसलिए भी है कि उनके व्यक्ति में शिक्षाविद् समाज-चिंतक, प्रशासक, अकादमीय विद्वान, सृजनात्मक निबंधकार और कहानीकार—सब एक साथ रहते हैं। इनमें से अगर कोई एक समयबद्ध संज्ञा हटानी पड़े तो मेरी नज़र में वह निस्संदेह प्रशासक की भूमिका ही होगी जो उन्होंने एनसीईआरटी के निदेशक के तौर पर निभाई थी। अगर कृष्ण कुमार उस पद को कभी सुशोभित न भी करते तब भी उनके महत्त्व में कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ता।
कृष्ण कुमार हमारे समय के उन विशिष्ट जन-बुद्धिजीवियों में हैं, जिनकी दृष्टि केवल प्रत्यक्ष राजनीतिक घटनाक्रमों पर जाकर नहीं ठहर जाती। उनके लेखन-चिंतन में वर्तमान की कोई घटना अगले-पिछले कारणों और संदर्भों के साथ उपस्थित होती है। इस कोण से देखें तो वह जन-बुद्धिजीवी की लगातार संकुचित होती परिभाषा को अपने योगदान और उपस्थिति से और विस्तृत कर देते हैं। उनका यह तहदार नज़रिया समकालीन समय में सूचनाओं के कचरे के बीच सही रास्ता ढूँढ़ने में मदद करता है। कहना न होगा कि पिछले तीन-चार दशकों के दौरान सार्वजनिक बौद्धिकता का अधिकांश प्रत्यक्ष और तात्कालिक लक्षणों की पहचान करने तक सीमित होता गया है। हम भूल गए हैं कि हमारे सामने प्रकट हो रहा यथार्थ अक्सर पीछे से चली आ रही प्रक्रियाओं और घटनाओं का संचित परिणाम भी होता है। कृष्ण कुमार के यहाँ यह शायद इसलिए संभव होता है, क्योंकि वह चीज़ों को ठहरकर देखते हैं। उनका मंतव्य सत्ता की कृपा और समीकरणों के बजाय समाज के मानचित्र से पोंछ दिए गए इलाक़ों की चिंता से तय होता है।
कृष्ण कुमार की किताबों, उनके सामयिक लेखों और आजकल यूट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों पर उपलब्ध उनके साक्षात्कारों से गुज़रते हुए; मैं अक्सर इस सोच में पड़ जाता हूँ कि उनके लेखन में वह क्या चीज़ है, जो अपनी ओर खींचती है। किसी चर्चा के दौरान या लिखते-पढ़ते उनकी कोई उक्ति या अंतदृष्टि कुछ इस तरह याद आती है कि काश! उस समय वह उद्धरण नोट कर लिया होता?
कई बार लगता है कि शिक्षा उनके लिए एक ऐसी विशालकाय खिड़की है, जहाँ से उन्हें पूरे समाज का उच्चावच्च नज़र आता है। इसलिए, जब हम उनका शिक्षा के किसी ख़ास पहलू पर केंद्रित लेख पढ़ रहे होते हैं, तब भी अपने इतिहास के अनुत्तरित प्रश्नों और वर्तमान में संसाधनों की उपलब्धता के सामाजिक असंतुलन की छवियों को देख रहे होते हैं। कृष्ण कुमार के लेखन की एक बड़ी सिफ़त यह है कि उनके किसी लेख, निबंध, संस्मरण या छोटी से छोटी सामयिक टिप्पणी को पढ़ते हुए भी पाठक उस परिघटना की व्यापक पृष्ठभूमि, पूर्वापर सूत्रों, समाज में शक्ति के केंद्रों और संरचनाओं से कुछ इस तरह परिचित होता चलता है कि वह परिघटना उसके लिए एक अनुभूत तथ्य बन जाती है। समझ के संप्रेषण का यह एक ऐसा तरीक़ा है, जो पाठक को अपरिचित या अपठित ज्ञान से आतंकित करने के बजाय उसे सार्वजनिक अनुभवों की दुनिया और उसकी विसंगतियों से परिचित कराता है। मसलन, अपनी बहुपठित पुस्तक ‘राज, समाज और शिक्षा’ के पहले अध्याय में राज्य, समाज, परिवार तथा शिक्षा व्यवस्था के विशाल परिसर में बच्चे की स्थिति और स्थान की शिनाख़्त करते हुए कृष्ण कुमार अपना बुनियादी वक्तव्य यहाँ से शुरू करते हैं :
‘‘शिशु के लालन-पालन में समाज और राजनीतिक सत्ता की भूमिका लगातार एक होती जा रही है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं, जिसमें सामूहिक जीवन को परिभाषित करने की ज़िम्मेदारी लोगों के हाथ में नहीं है। सामूहिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण भाग बच्चों का विकास है, जिसे परिभाषित करने का अधिकार संपूर्णतः स्कूल के पास है। स्कूल स्वयं हमारे समाज के शासक वर्ग के एक प्रमुख घटक-नौकरशाही के नियंत्रण में है। बच्चों का भोजन, उनके खिलौने, उनकी पत्रिकाएँ और किताबें हमारे शहरी मध्यवर्ग के नियंत्रण में हैं...’’ (पृष्ठ : 13)
कहना न होगा कि कृष्ण कुमार इन शुरुआती पाँच वाक्यों में स्पष्ट संकेत कर देते हैं कि शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था में साधारण बच्चे अपने लिए क्या और कितनी उम्मीद कर सकते हैं।
इस क्रम में वह भारतीय समाज के अंतर्विरोधों की एक इतिहासकार के तौर पर पड़ताल करते हुए कहते हैं कि भारत में स्वतंत्रता का आंदोलन समाज के बहुत-से तबक़ों और शिक्षा जैसे अहम क्षेत्रों को संबोधित किए बग़ैर भी सफल हो गया।
कृष्ण कुमार का कहना है कि गांधी जी शिक्षा के प्रश्न को स्वतंत्रता-आंदोलन में शामिल करना चाहते थे। एक सीमा तक वह इसमें सफल भी हुए। लोगों को यह बात समझ आई कि उच्च शिक्षा का पूरा तंत्र औपनिवेशिक प्रतिष्ठान की सेवा में लगा है, परंतु अंतत: यह मुहिम अस्थायी सिद्ध हुई। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की योजना औपनिवेशिक सत्ता द्वारा स्थापित प्रतियोगी शिक्षा के आगे कमज़ोर साबित हुई और आज़ादी के चंद बरसों के भीतर बुनियादी शिक्षा के द्वारा समाज के पुनर्निर्माण का विचार कुछ ‘नमूना-संस्थाओं’ की भेंट चढ़ गया। इसके बाद वही शिक्षा-पद्धति परवान चढ़ती चली गई जो शासक और शासितों के विभाजन को मज़बूत करती थी। (वही, 43)
दूसरी बात, कृष्ण कुमार का अकादमीय शैक्षिक लेखन भी एक संवाद की तरह चलता है। उसे पढ़ते हमेशा ऐसा लगता है कि हम किसी बातचीत में भाग ले रहे हैं। इस बात को थोड़ा फैलाकर देखें तो उनके यहाँ प्रस्तुत विषय अपनी समस्त जटिलताओं के बावजूद कभी दुर्बोध नहीं होता। पाठक बहुत जल्दी उसमें अपने प्रवेश के बिंदु खोज लेता है।
तीसरे—और यह उनकी बौद्धिक निष्ठाओं की निरंतरता का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है कि कृष्ण कुमार शिक्षा के विज्ञापित आदर्शों और उसकी संरचनात्मक विसंगतियों पर लगभग चार-पाँच दशकों से नियमित लिखते आ रहे हैं। यह एक ख़ासी लंबी अवधि है, जिसमें बहुत-से कथित अग्नि-वर्षक विद्वान भी ट्रैक बदल लेते हैं। लेकिन कृष्ण कुमार जिन सवालों पर पैंतालीस बरस पहले विचार कर रहे थे, उनके समाधान को लेकर आज भी उतने ही फ़िक्रमंद हैं। मसलन, यह एक दुर्लभ बात है कि आज से सैंतालीस वर्ष पहले 1978 में छपी अपनी पूर्वोद्धृत किताब ‘राज, समाज और शिक्षा’ में कह रहे थे कि स्कूल भले ही समाज के अंदर स्थित होता हो, परंतु स्कूल में समाज का प्रवेश नहीं हो पाता। उनके मुताबिक़ इसका परिणाम यह हुआ है कि :
‘‘स्कूल की चहारदीवारी केवल सुरक्षा का साधन नहीं रह गई है, वह बचपन और सामाजिक जीवन को एक-दूसरे से अलग रख नेवाली सीमा बन गई है। चहारदीवारी के भीतर ऐसी जानकारी बच्चों को दी जाती है, जिसका उनके दैनंदिन जीवन से संबंध नहीं होता। कहने को स्कूल बच्चों की भाषा का विकास करता है, पर भाषा जीवन के सतत अनुभव से ही अर्थ ग्रहण करती है। भारतीय स्कूल पर पाठ्य-पुस्तकों का इतना कड़ा नियंत्रण है कि स्कूल के बाहर स्थित समाज की जीवंत भाषा कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाती।’’ (पृष्ठ : 21)
यहाँ ग़ौर करने की बात यह है कि चार-पाँच बरस पहले के अपने एक इंटरव्यू में कृष्ण कुमार लगभग वही बात कह रहे थे कि छह साल तक के बच्चों में एक ऐसी स्वाभाविक ऊर्जा होती है, जो उन्हें हर चीज़, हरेक गतिविधि, पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं आदि के प्रति जिज्ञासा से भरे रखती है। इस उम्र में बच्चे स्कूल के अनुशासन को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन, शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था में बच्चे को एक उत्पादक मशीन का पुर्ज़ा बना दिया गया है। इसमें उसकी स्वाभाविक क्षमताओं और कल्पनाशीलता के लिए कोई जगह नहीं है। सच तो यह है कि इसमें उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों और रुझानों को हतोत्साहित किया जाता है।
लगभग बीस मिनट के उस साक्षात्कार में कृष्ण कुमार बच्चे के बनते हुए मानस के प्रति शिक्षा-व्यवस्था की क्रूरता पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि बच्चे के स्वभाव और स्कूल की व्यवस्था में एक अंतर्विरोध है। स्कूल का ज़ोर इस पर रहता है कि बच्चा क्लास में बताई जा रही बातों को ध्यान से सुनें, सीखे और याद करे। लेकिन बच्चे का ध्यान बदलती हुईं ऋतुओं, पेड़ों, चींटियों, कीड़े-मकोड़ों आदि जैसी कौतुक भरी चीज़ों पर रहता है। इस उम्र के बच्चे में असीम जिज्ञासा होती है। वह हवा में हो रहे परिवर्तन को अपनी त्वचा पर महसूस करना चाहता है। भागना, दौड़ना चाहता है।
यह संयोग नहीं है कि 2005 में जब एनसीईआरटी के निदेशक के तौर पर कृष्ण कुमार को शिक्षा के पीछे से चले आ रहे ढाँचे में एनसीएफ़ (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या) के ज़रिये सार्थक हस्तक्षेप करने का अवसर मिला तो उसमें बात का ख़याल रखा गया कि बच्चे की घरेलू और आस-पड़ोस की ज़िंदगी कक्षा में आए। बच्चे को स्कूल की खिड़की से दिख रहा संसार अध्यापक के लिए भी महत्त्वपूर्ण बने। स्कूल में पाठ्यक्रम के तहत चल रही गतिविधियों को बच्चों की सहज क्रियाओं से जोड़ा जाए।
एक तरह से देखें तो यह सोच अपने बौद्धिक जीवन के शुरूआती वर्षों में हासिल की गई; उस अंतर्दृष्टि का प्रतिफलन कही जा सकती है, जब कृष्ण कुमार यह लिख रहे थे :
‘‘अपने आस-पास के यथार्थ से अपना रिश्ता न समझ पाने वाला व्यक्ति लगातार बेगाना होता चला जाता है और अपने बेगानेपन का स्रोत न समझ सकने के कारण अंततः अपनी सुरक्षा किसी व्यापक, निर्वैयक्तिक संरचना को समर्पण में पाता है। सभ्यता के विकास की एक स्थिति में यह व्यापक, निर्वैयक्तिक संरचना प्रायः अध्यात्म होती है; आज वह लगभग सदैव राजनीतिक सत्ता होती है। (वही)
ख़ालिस शिक्षा से संबंधित इन उद्धरणों में कृष्ण कुमार एक ऐसे सांस्कृतिक चिंतक के रूप में भी प्रकट होते हैं, जिसका सरोकार केवल अपने चुने हुए अकादमीय क्षेत्र तक सीमित नहीं है। वह शिक्षा पर बात करते हुए समाज, साहित्य, सत्ता के स्रोत, उसकी वर्गीय बनावट, संविधान द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों और उनकी बेक़दरी के लिए ज़िम्मेदार प्रक्रियाओं की निशानदेही तक जाते हैं। मसलन, बच्चों की सांस्कृतिक अभिरुचि के निर्माण और उनके समाजीकरण में खिलौनों की भूमिका पर बात करते हुए वह उस चुप्पी प्रक्रिया को लक्षित करते हैं, जिसमें गुड्डे-गुड़िया का खेल लड़कियों को दांपत्य जीवन के घरेलू पक्ष के लिए तैयार करता जाता है। गुड़ियों की वेशभूषा, उनकी सजावट और शृंगार उन्हें बचपन में ही वधू के पारंपरिक सौंदर्य का अभ्यस्त बना देने का प्रशिक्षण होता है। खिलौनों में निहित इस सांस्कृतिक बोध की व्याख्या करते हुए कृष्ण कुमार कहते हैं :
‘‘बाज़ार में बिकनेवाली गुड़िया हमेशा सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए तैयार प्रतियोगी और बनी-ठनी वधू का मिला-जुला रूप होती है। प्लास्टिक की गुड़ियों में मेम की आकृति बहुत प्रचलित है; सुनहरे बाल, लाल होंठ और फ्रॉक में लैस गुलाबी बदनवाली फ़िरंगी मेम आज भी भारतीय कल्पना के नारी-रूपों में से एक है। बाज़ार में आने वाली गुड़ियों के दोनों रूप-वधू और मेम हमारी लड़कियों की कल्पना को विकृत करने में परंपरापोषी वयस्कों को मदद देते हैं। वे उन्हें उस समाज को ज्यों का त्यों क़ुबूल कर लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं, जिसमें नारी के ये दो ही रूप हैं—सर्वगुणसंपन्न सौंदर्यवती गृहवधू और गुणहीना उच्छृंखल आधुनिका।’’ (र.स.शि., पृष्ठ : 133)
उनका यह सांस्कृतिक चिंतन हमें उनकी एक अन्य विचारोत्तेजक किताब ‘चूड़ी बाज़ार में लड़की’ की इस अन्वीक्षा में भी मिलता है :
‘‘स्त्री के शरीर पर हर गहने का स्थान पुरुष के निर्देशन में बने संस्कृति के मानचित्र के अनुसार निर्धारित हुआ है; गहने को पहने खड़ी या बैठी स्त्री मात्र एक माध्यम है। उसकी देह एक सार्वजनिक कैनवास है जिस पर पुरुष-सत्ता में निहित कल्पना, सौंदर्य-दृष्टि और कौशल इस तरह अभिव्यक्ति पाते हैं कि एक निश्चित नाम से पहचानी जाने वाली औरत ग़ायब हो जाती है और सिर्फ़ देह की सामान्यता बची रह जाती है। स्त्री जब कोई गहना पहन या उतार रही होती है तो इन दोनों कामों में वह संस्कृति की एक समर्पित, और अपनी भूमिका व हैसियत के प्रति चौकस, सेविका की भाँति व्यवहार कर रही होती है। (चूड़ी का चिह्नशास्त्र, पृष्ठ : 67)
बहरहाल, जैसा कि हमने इस टिप्पणी की शुरुआत में इशारा किया था; कृष्ण कुमार के भीतर एक कहानीकार भी रमता है जो कहानी के प्रचलित ढर्रे का अनुसरण करने के बजाय समाज के भू-गर्भ में चलती गतियों का आरेखण करता है। उनकी एक ज़बरदस्त कहानी— ‘प्रतिकार’ कभी ‘हंस’ में छपी थी जो बाद में ‘काठगोदाम’ (2018) शीर्षक उनके कथा-संग्रह में भी दिखी थी। इस संग्रह में उपरोक्त कहानी के अलावा ‘बाँस का कीड़ा’, ‘साँप’, ‘शरद की दोपहर’, ‘सुबह की सैर’ और ‘काठगोदाम’ जैसी अनेक नायाब कहानियाँ हैं, जिनमें समाज के बाहरी और व्यक्ति के भीतरी यथार्थ की बहुत सूक्ष्म और ऐसी नन्हीं छवियाँ दर्ज हुई हैं जो कहानियों के स्थापित ढाँचे में बहुत कम दिखाई देती हैं। लेकिन उनके कहानीकार पर शायद ही किसी ने ठीक से चर्चा की है। यह शायद इसलिए भी है कि अंतर-अनुशासनिकता के तमाम दावों के बावजूद स्थिति यह है कि अकादमिक जगत की तरह साहित्य के दरवाज़ों पर भी टीसी (टिकट-चेकर) बैठे हैं।
~~~
समादृत शिक्षाविद् कृष्ण कुमार इस बार के ‘हिन्दवी उत्सव’ में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित हैं। ‘हिन्दवी उत्सव’ से जुड़ी जानकारियों के लिए यहाँ देखिए : हिन्दवी उत्सव-2025
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
12 जून 2025
‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही’
‘बॉर्डर 2’ का विचार सुनते ही जो सबसे पहला दृश्य मन में कौंधा, वह बालकनी में खड़े होकर पिता का कहना था—‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही।’ इस वाक्य में सिर्फ़ एक अभिनेता का अवसान नहीं था, एक पूरे युग क
29 जून 2025
‘बिंदुघाटी’ पढ़ते तो पूछते न फिरते : कौन, क्यों, कहाँ?
• उस लड़की की छवि हमेशा के लिए स्टीफ़न की आत्मा में बस गई, और फिर उस आनंद में डूबा हुआ पवित्र मौन किसी भी शब्द से नहीं टूटा... आप सोच रहे होंगे कि यहाँ किसी आशिक़ की किसी माशूक़ के लिए मक़बूलियत की बा
14 जून 2025
बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल!
‘बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल’—यह नब्बे के दशक में किसी पल्प साहित्य के बेस्टसेलर का शीर्षक हो सकता था। रेलवे स्टेशन के बुक स्टाल्स से लेकर ‘सरस सलिल’ के कॉलमों में इसकी धूम मची होती। इसका प्रीक्वल और सीक्वल
10 जून 2025
‘जब सोशल मीडिया नहीं था, हिंदी कविता अधिक ब्राह्मण थी’
वर्ष 2018 में ‘सदानीरा’ पर आपकी कविता-पंक्ति पढ़ी थी—‘यह कवियों के काम पर लौटने का समय है’। इस बीच आप फ़्रांस से लौटकर आ गए। इस लौटने में काम पर कितना लौटे आप? 2018 में जब यह कविता-पंक्ति संभव हुई
20 जून 2025
8/4 बैंक रोड, इलाहाबाद : फ़िराक़-परस्तों का तीर्थ
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एम.ए. में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी मेरे मित्र बन गए। मैं उनसे उम्र में छोटा था, लेकिन काव्य हमारे मध्य की सारी सीमाओं पर हावी था। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। उनका नाम वीरेंद्र