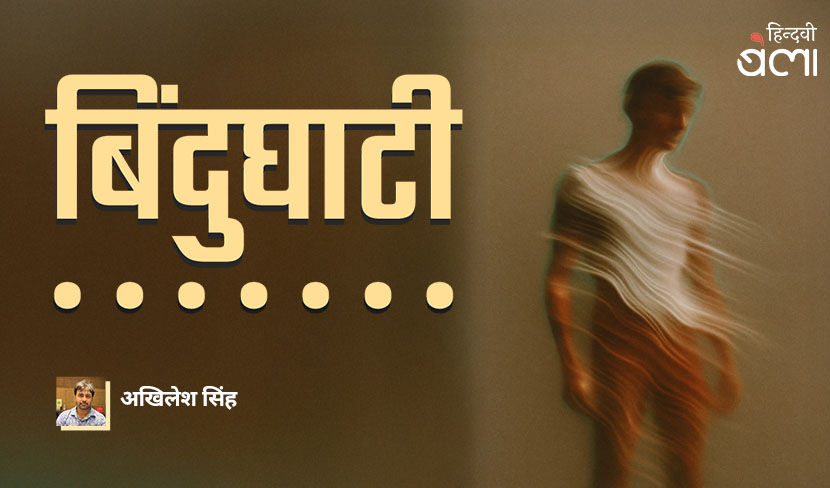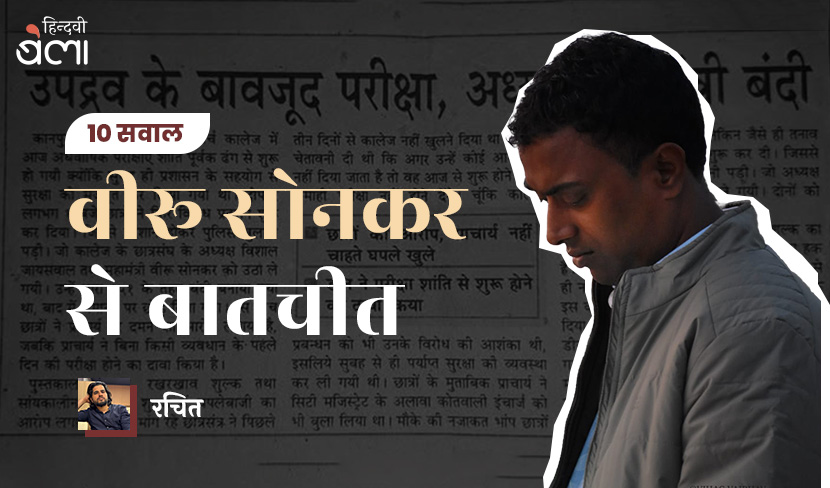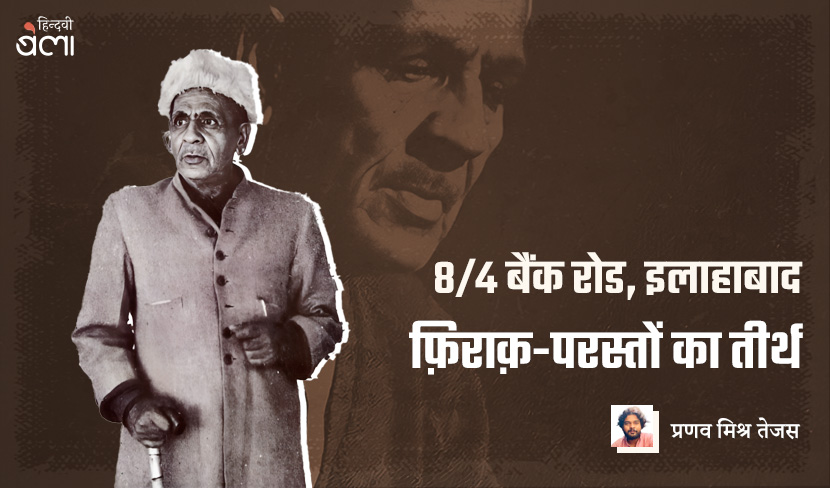अतीत का अँधेरा और बचकानी ख़्वाहिशें
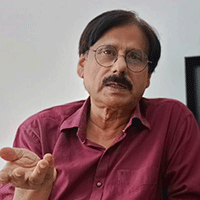 ख़ालिद जावेद
25 मई 2025
ख़ालिद जावेद
25 मई 2025
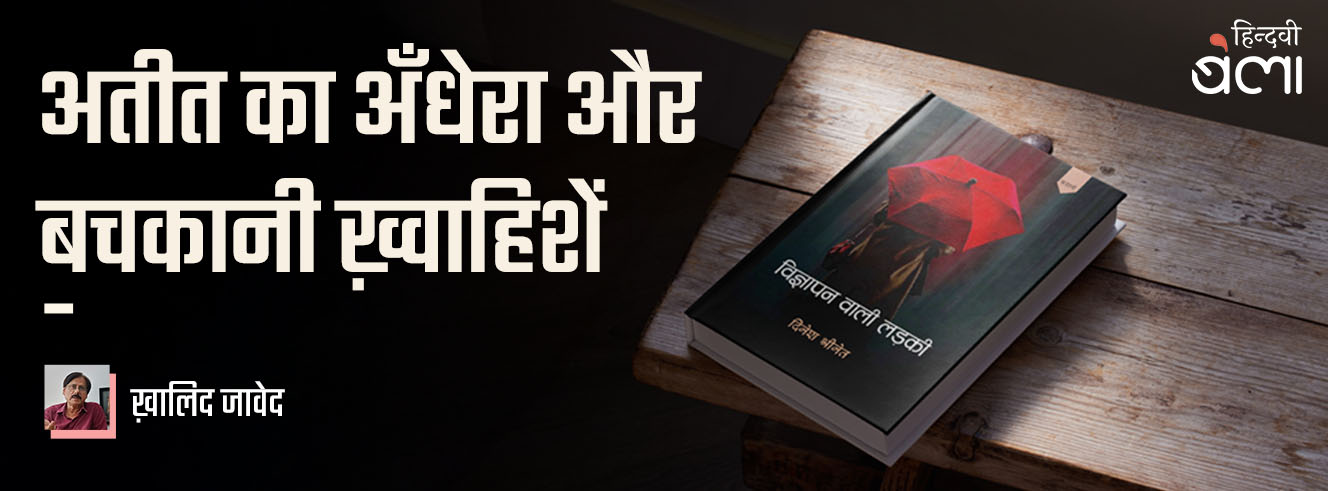
दिनेश श्रीनेत की कहानियों का संग्रह प्रकाशित होकर सामने आया है और मैं ख़ुशी के साथ एक अजीब से एहसास से भी सराबोर हूँ। मैं इस एहसास को कोई नाम देने में ख़ुद को लाचार समझता हूँ। मगर इस एहसास के केंद्र या एपिसेंटर (Epicenter) में कुछ ऐसा है, जिसे मैं बयान कर सकता हूँ और यह भी जानता हूँ कि इस एहसास का ख़ामोश ज्वालामुखी इसी स्थान से पैदा होकर धुंध का एक बवंडर मेरे ज़ेहन के चारों तरफ़ पैदा कर रहा है। मगर इस एपिसेंटर तक पहुँचने के लिए मुझे सत्ताईस वर्ष पुराने अतीत के अँधेरे या धुंध भरे रास्तों पर वापस लौटना होगा।
तब मैं बरेली कॉलेज में दर्शन विभाग में लेक्चरर था। हल्के-हल्के जाड़ों की एक उदास दोपहर थी। मैं स्टाफ़ रूम में बैठा हुआ, अपनी क्लास का इंतज़ार कर रहा था और तभी मेरे विभाग के साथी त्रिपाठी जी के साथ एक नौजवान वहाँ दाख़िल हुआ। त्रिपाठी जी उस ज़माने में बरेली कॉलेज में, मेरे अकेले दोस्त हुआ करते थे (अब तो ख़ैर टेम्स नदी में बहुत पानी बह चुका है)।
त्रिपाठी जी ने नौजवान का मुझसे परिचय कराया, “ये दिनेश श्रीनेत हैं। बरेली में अमर उजाला में बतौर रिपोर्टर इनकी नियुक्ति हुई है। ये एजुकेशनल न्यूज़ कवर करेंगे।”
हम दोनों ने एक-दूसरे से हाथ मिलाया। फिर कुछ देर बाद चाय पीने के लिए हम लोग बरेली कॉलेज के उस गेट पर गए, जिसके सामने पागलख़ाने की दीवार है। वहीं राधे का मशहूर होटल था, जिसकी चाय के साथ नमकपारे और गुलाब जामुनों की भी बहुत शोहरत थी। बातचीत के दौरान अचानक हिंदी-साहित्य का ज़िक्र हुआ और फिर बात निर्मल वर्मा तक पहुँच गई। और फिर मेरी दुनिया बदल गई। त्रिपाठी जी तो कुछ देर में चले गए, मगर हम दोनों सिर्फ़ निर्मल वर्मा के बारे में बातें किए जा रहे थे। शायद पागलों की तरह। और हमारे सामने अब सिर्फ़ पागलख़ाने की काली दीवार थी, जिससे लगकर गुज़रने वाला ट्रैफ़िक अपना शोर पता नहीं कहाँ गिराकर या छोड़कर चला आया था।
तो यह थी दिनेश श्रीनेत से मेरी पहली मुलाक़ात। 25 नवंबर 1998 की यह उदास मगर बहुत ही बामानी दोपहर आगे न जाने कितनी दोपहरों से जा मिली और सिर्फ़ दोपहर ही नहीं, रातों में भी यह दोपहर एक रोशन सुरंग की तरह गुज़रती रही। दिनेश, जैसे आज हैं वैसे ही कल थे। सत्ताईस साल पहले भी इतने ही संजीदा मगर ख़ुशमिज़ाज और मुस्कुराहट से भरा हुआ चेहरा। मैंने संजिदगी और ख़ुशमिज़ाजी का ऐसा संगम बहुत कम ही देखा है। उस ज़माने में भी ख़ुश लिबास और आज भी ख़ुश लिबास। गुज़रते हुए ज़माने ने उनके अंदर कुछ बदल दिया हो, वह अलग बात है मगर बाहर से उनकी शख़्सियत का जादू आज भी पहले ही की तरह बरकरार है। ठीक है कि कहीं-कहीं बढ़ती हुई उम्र ने उनकी कशिश को ज़्यादा कर दिया है। उम्र बढ़ते रहना एक तरह की सुंदरता है, जिसे सिर्फ़ महसूस किया जा सकता है।
मेरे और दिनेश के दरमियान न जाने कितना कुछ मुश्तरक था। ख़याल, पसंद, कपड़े, खाना, बातचीत, अदब और फ़िल्में, यहाँ तक कि इब्न-ए-सफ़ी भी। निर्मल वर्मा तो ख़ैर हम दोनों के दरमियान एक ऐसे पुल की तरह थे, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। वह बरेली से लखनऊ गए, कानपुर गए, इलाहाबाद गए, बैंगलोर गए, दिल्ली आए। मैं बरेली से दिल्ली आ गया। मगर वह न ख़त्म होने वाला पुल कभी न तो टूटा और न ही कमज़ोर हुआ।
ये सारी कहानियाँ उन्होंने मुझे लिखते ही सुनाई हैं। कुछ कहानियाँ बरेली में और कुछ बहुत बाद में दिल्ली आने के बाद। इन कहानियों को सुनाने और इन पर बातचीत करने के ठिकाने विभिन्न प्रकार के थे और कभी-कभी बहुत अजीब भी। मसलन जब दिनेश राम वाटिका कॉलोनी में एक कमरा किराए पर लेकर रहते थे—मैं, ज़ीनू (मेरी बेटी) को प्ले स्कूल छोड़ कर सुबह-सुबह उनके घर पर पहुँच जाता था। वह सख़्त गर्मी और उमस के दिन थे। उनके कमरे में सन्नी का छोटा-सा काला टेबल फ़ैन एक स्टूल पर रखा रहता था, जो आँधी का सा शोर पैदा करता था, मगर उस आँधी की हवा जिस्म को कम और दीवारों को ज़्यादा लगती थी। उस पंखे से घबराकर हम राम वाटिका के पिछले गेट से निकल कर उसी गली में आ जाते थे, जहाँ सड़कों की मरम्मत और उनके टायरों के पंक्चर जोड़ने का काम होता था। वहीं चाय का एक छोटा-सा ढाबा था। हम दोनों वहीं एक तिपाई पर बैठ जाते थे, जो धूल और ख़ाक से अटी रहती थी। हम वहाँ गिलास में उतारी गई चाय पीते थे और एक-एक बन भी खाते थे। उस बन में टायरों की रबर और मोबिल ऑयल की बू आती थी। हम बन पर बहुत बात करते थे कि वह किस तरह स्लाइस और बिस्किट से अलग पहचान रखता है। ये बातें एक तरह से बकवास ही होती थीं, मगर सुबह-सुबह अपनी-अपनी आँखों में जमी रह गई नींद को खुरचने के लिए शायद यह बकवास ज़रूरी थी। बहुत बाद में जब दिनेश ने अपनी लाजवाब कहानी ‘विज्ञापन वाली लड़की’ लिखी, तो उसमें यह ‘बन’ लगभग एक किरदार या ‘मोटिफ़’ की तरह उभर कर सामने आया।
फिर गर्मी और उमस के दिन ख़त्म होते थे और बारिश शुरू हो जाती थी। उन दिनों बरेली में लगातार एक-एक हफ़्ता बारिश होती रहती थी। हम उस बारिश पर भी बेतुकी बातें करते रहते थे और कैंट में बहने वाली पुरानी नदी नकटीया के किनारे बैठकर या पुल पर खड़े होकर बारिश का मंज़र देखते थे। दिनेश श्रीनेत की कहानियों में जो धीरे-धीरे लगातार गिरती हुई—बारिश के मंज़र देखने को मिलते हैं, वह मेरे हवास व इदराक के लिए अजनबी नहीं हैं बल्कि बहुत अपने-अपने से लगते हैं। दिनेश की भाषा ख़ुद भी धीरे-धीरे होती हुई बारिश की तरह ही है। वह गरज चमक और सैलाब जैसी भाषा नहीं है, जो पढ़ने वाले को बहा ले जाए। धीमे-धीमे गिरती हुई लगातार बारिश वजूद को भिगोती है, जिस्म को नहीं।
कुछ कहानियाँ मेरे बरेली वाले घर की पुरानी बैठक में उन्होंने मुझे सुनाई थीं। यह वह ज़माना था, जब मैं और दिनेश दिन में कम-से-कम दो बार ज़रूर मिला करते थे। ज़्यादातर दोपहर में और फिर अक्सर शाम को। दिनेश वैसे तो अख़बार में बतौर जर्नलिस्ट काम करते थे, मगर साहित्य उनका ओढ़ना-बिछौना था। उन्होंने अपनी पत्रकारिता को अपने अंदर बसने वाले एक लेखक और कवि हृदय पर हावी न होने दिया। वह फ़िल्मों के बहुत शौकीन हैं और फ़िल्म की सूझ-बूझ के साथ-साथ उसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर उनकी पकड़ बहुत मज़बूत है। हम कभी बर्गमैन और तारकोवस्की की फ़िल्मों पर बात करते थे और कभी-कभी किसी मैटनी शो में ‘अक्स’ और ‘हम दिल दे चुके सनम’ के साथ नटराज टॉकीज में ‘मैट्रिक्स’ देखने भी निकल जाते थे। दूर वीरान से फ़ौजी छावनी के इलाक़े में बने हुए, इस रहस्यमय गॉथिक टॉकीज में फ़िल्म देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। कोई हैरत नहीं कि दिनेश श्रीनेत की सिनेमा पर लिखी दो किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं।
दिनेश को यात्रा-वृत्तांत लिखने पर भी कमाल हासिल है। मैहर पर जो उनका यात्रा-वृत्तांत है, उसकी भाषा की तारीफ़ शमीम हनफ़ी करते नहीं थकते थे। दरअस्ल दिनेश की लेखनी की सबसे बड़ी ताक़त उनकी भाषा ही है। दिनेश की लिखी हुई एक अख़बारी रिपोर्ट या स्टोरी तक दूसरे पत्रकारों से बिल्कुल अलग है। उनके लेख चाहे वह सिनेमा पर हों या साहित्य पर या सामाजिक राजनीतिक मसलों पर, हर जगह उनकी अपनी अनोखी मगर दिल में उतर जाने वाली भाषा मौजूद रहती है। तो फिर ज़ाहिर है कि जब वह अपने अस्ल मैदान यानी कथा कहने में आकर अपना क़लम उठाएँगे तो यह भाषा जर्नलिज्म या एकेडमिक डिसिप्लिन की बंदिशों से आज़ाद होकर क्या क़यामत ढाएगी, इसका अंदाज़ा हर कोई लगा सकता है।
शायद यह भाषा उनकी आत्मा और ज़मीर के नाप की ज़बान है। दिनेश नाम निहाद ‘लेफ़्ट’ लिखने वाले फ़ैशनेबल लेखक नहीं हैं और इसीलिए कभी-कभी ‘कलावादी’ का लेबल भी उन पर चस्पाँ कर दिया जाता है। (हमने ‘कला’ को ‘वाद’ के साथ मिलाकर शायद एक अदबी गाली की ईजाद कर ली है), मगर दिनेश की इंसान-दोस्ती और रोशन-ख़याली हर किस्म के भेदभाव से पाक ज़हन और उसका जुर्रत आमेज़ अमली इज़हार और उनके आत्मसम्मान ने मिलकर अपनी शख़्सियत के इज़हार का जो रास्ता चुना है; वह यही भाषा है। एक ज़िंदा, थरथराती हुई भाषा जो लिखते वक़्त काग़ज़ पर ऐसे ही गिर रही हो—जैसे वहाँ हल्की-हल्की लगातार बारिश हो रही हो। इस भाषा से उनका सफ़्हा भीगता जाता है। यह भाषा, यह बारिश, जिसमें उदासी, मौत, तन्हाई और इंसान मिलकर एक ऐसे त्रिकोण की तामीर करते हैं, जो बहुत बामानी है। इस त्रिकोण में किसी सस्ते से सियासी या समाजी नारे के लिए कोई जगह नहीं है। यह ‘इंसान’ से मुताल्लिक़ भाषा है। इंसान के वजूद की गहरी परतों को खंगालती हुई भाषा है। और इंसान का वजूद अपने अहद और अपने अहद के मसाइब से कट कर ज़िंदा नहीं रह सकता। दिनेश श्रीनेत की कहानियाँ इस सब की एक ख़ामोश testimony हैं।
सन् 2000 में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग से मुंसलिक हो गया। तब मैं छात्र मार्ग पर एक किराए के कमरे में रहता था, जो पाँचवीं मंज़िल पर था। लिफ़्ट नहीं थी। एक गोल चक्करदार भूतिया ज़ीना चढ़कर मैं कमरे तक पहुँचता था। वह बहुत अकेलेपन का ज़माना था। मुझे वहाँ पहुँचे मुश्किल से एक हफ़्ता गुज़रा होगा कि दिनेश श्रीनेत मुझसे मिलने दिल्ली आ गए। मेरे लिए गोया ईद हो गई। उस कमरे में बैठकर हमने फिर ढेर सारी बातें कीं जो निर्मल वर्मा के साथ-साथ मोहन राकेश और शानी के बारे में भी थीं। कुछ फ़ासले पर मॉडल टाउन में बलराज मेनरा रहते थे। हर शाम को हम दोनों उनसे मिलने उनके घर जाया करते जो दरअस्ल टीबी अस्पताल का सरकारी क्वार्टर था। बलराज मेनरा को दोस्तोयेवस्की और आयन रैंड से इश्क़ था। रूसी अदब दिनेश श्रीनेत ने भी बहुत पढ़ रखा था। वहाँ बलराज मेनरा से रूसी और फ़्रांसीसी अदब पर ख़ूब बहसें होती थीं।
दिनेश हमेशा मुझसे मिलने दिल्ली आते रहे। उस ज़माने में भी जब वह लखनऊ और फिर बैंगलोर चले गए थे। 2005 में जनवादी लेखक संघ ने मेरी कहानी ‘तफ़री की एक दोपहर’ का पाठ कराया था, जिसके बाद कहानी पर चर्चा करने के लिए असग़र वजाहत, शमीम हनफ़ी, रिज़वानुल हक़ और दिनेश श्रीनेत का नाम तय हुआ था। दिनेश मेरी कहानी पर बोलने के लिए कानपुर से दिल्ली आए थे। दिल्ली में मेरे सारे दोस्त उनके भी दोस्त बन गए। मसलन खुर्शीद अकरम, अकरम खावर, रिज़वानुल हक़, फ़रहत एहसास, नजमा रहमानी, दिलीप शाक्य और अनवर जमाल। शमीम हनफ़ी और शम्सुर रहमान फ़ारुकी भी दिनेश को बहुत पसंद करते थे। दिल्ली में हम कई बार साथ-साथ उदय प्रकाश से भी मिले, जो उस ज़माने में रोहिणी के एक फ़्लैट में रहते थे। निर्मल वर्मा से मैं कई बार मिला। उन्होंने मेरी किताब का फ़्लैप भी लिखा था। निर्मल वर्मा से दिनेश श्रीनेत का पत्र-व्यवहार बहुत पहले से था। मगर इत्तेफ़ाक़ यह हुआ कि हम दोनों साथ-साथ कभी निर्मल वर्मा से न मिल सके। दिल्ली में उर्दू के मशहूर शायर सलाहुद्दीन परवेज़ भी दिनेश को बहुत पसंद करते थे। दिनेश के साथ घूमना दरअस्ल एक महफ़िल की तरह था। यही हाल बरेली का था। बरेली में भी जो मेरा दोस्त था, वह उनका दोस्त भी था। शायरों में शारिक कैफ़ी, सरदार ज़िया, ख़ान जमील और अदीबों में मशहूर फ़ोटो जर्नलिस्ट और लेखक प्रभात या फिर कुंवर सतीश चंद्र जैसे दोस्त और डॉक्टर राजेश शर्मा जैसे किताबों और संगीत के प्रेमी शामिल थे। यह सब एक महफ़िल सजाने की तरह था। लेकिन मैं और दिनेश सिर्फ़ इन महफ़िलों के ही साथी न थे। हम महफ़िलों के बाद के सन्नाटे के भी गवाह रहे हैं।
मुझे दिल्ली से बरेली तक रात में एक खटारा बस में सफ़र करने का इत्तेफ़ाक़ हुआ। मेरे साथ दिनेश भी थे। हमने उस बेहद तकलीफ़देह सफ़र में, किताबों पर और लेखकों पर इतनी बातें की थीं और उन बातों के करने में ख़ुशी इतनी थी कि पता ही नहीं चला कि रात के ढाई बजे, सात घंटे का सर में दर्द कर देने वाला सफ़र तय कर के हम कब बरेली के रोडवेज बस अड्डे पर हँसते खेलते उतर गए। बिल्कुल तर व ताज़ा और ख़ुश व ख़ुर्रम। और मुझे आज भी यकीन है कि आप सही मायने में सिर्फ़ अपने सच्चे दोस्तों के साथ ही ख़ुश रह सकते हैं। वरना इस मनहूस दुनिया में ख़ुश रहने के लिए कोई मक़ाम नहीं बचा है।
सत्ताईस साल के इस तवील सफ़र में कभी कोई ऐसा पड़ाव नहीं आया, जब हमारे रिश्तों के बीच हल्की-सी भी खटास पड़ी हो। दिनेश जितने अच्छे लेखक हैं, उतने ही अच्छे और बड़े ज़र्फ वाले इंसान भी हैं। उन्होंने हर मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया। मुझे जब भी उनसे कोई काम पड़ा, उन्होंने दोबारा कहने का मुझे मौक़ा न दिया और फ़ौरन ही कर के दे दिया। ऐसे दोस्तों का शुक्रिया भी अदा किया जाए तो किस तरह!
दिनेश श्रीनेत को अदब से लगाव विरासत में मिला है। उनकी वालिदा को नॉवेल, कहानियाँ और अदबी और फ़िल्मी रसाले पढ़ने का बहुत शौक़ था। उनकी अपनी एक छोटी-सी लाइब्रेरी थी। वह हर वक़्त पढ़ती रहती थीं। दिनेश ने आँख इन किताबों के दरमियान ही खोली थी। 2006 में उनकी वालिदा का इंतिक़ाल हुआ था। अजीब इत्तेफ़ाक़ है कि उन्हीं दिनों निर्मल वर्मा का भी इंतिक़ाल हुआ था। इस सानिहे से कुछ दिन पहले ही हम दोनों ने फ़ोन पर निर्मल वर्मा की लंबी कहानी ‘बीच बहस में’ पर एक लंबी गुफ़्तगू की थी। मुझे एहसास है कि मैं जो लिख रहा हूँ, उसमें कोई रब्त नहीं है, मगर आज जब दिनेश की कहानियों का संग्रह ‘विज्ञापन वाली लड़की’ प्रकाशित होकर मेरे हाथों में है, तो मैं जिस एहसास से दो-चार हूँ, वह महज़ इस किताब तक महदूद नहीं है। वह रचना और रचनाकार दोनों का अहाता कर लेता है। इस किताब पर मैं सिक्का बंद आलोचकों या पेशेवर तब्सिरा निगारों की तरह कुछ लिख पाने में ख़ुद को असमर्थ पाता हूँ। इस किताब के बहाने मैं माज़ी के अँधेरे, पुराने रास्तों को फिर से रोशन करने की एक बचकाना-सी ख़्वाहिश में गिरफ़्तार हूँ। अगर कोई किताब, किसी रास्ते को रोशन नहीं करती, अगर कोई किताब ख़ुद आपको ही अपनी भुलाई गई ज़िंदगी को याद नहीं दिलाती और अपने आप को फिर से दरयाफ़्त करने पर मजबूर नहीं करती तो मैं उसे ‘किताब’ नहीं समझता। हर लिखे गए ‘लफ़्ज़’, हर लिखे गए पैराग्राफ़ का मुक़द्दर ‘किताब’ बनना नहीं होता। चाहे वह दस हज़ार सफ़हात पर मुश्तमिल काग़ज़ों का ढेर ही क्यों न हो, जो बुक शेल्फ़ में पड़े-पड़े सिर्फ़ दीमकों को ही अपनी तरफ़ आने की दावत देता रहता है।
मगर सिर्फ़ 120 सफ़हात की यह ‘किताब’ वह अस्ल किताब है, जिसे पढ़ मैं ख़ुद को अज़-सरे-नौ (एक नई शुरुआत) तलाश करने के लिए निकल खड़ा हुआ हूँ। यानी अपनी ज़ात की खोजबीन का वसीला ‘विज्ञापन वाली लड़की’ है। इस मजमुए में सिर्फ़ पाँच कहानियाँ हैं—‘उड़न खटोला’, ‘विज्ञापन वाली लड़की’, ‘मात्र्योश्का’, ‘उजाले के द्वीप’ और ‘नीलोफर’। यह पाँचों कहानियाँ उन्होंने मुझे सुनाई थीं। अब पक्की रोशनाई में इसे छपा हुआ देखकर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यह सारी कहानियाँ इंसानी वजूद की परतों को बड़ी फ़नकारी के साथ खोलती हैं। यह कहानियाँ दुख, तकलीफ़ और मौत के चारों तरफ़ बुनी गई हैं। यह दुख और तकलीफ़ इंसान के किसी मख़सूस अमल का नतीजा नहीं है, यह दुख तो ‘इंसान’ होने की ‘वजूदी सूरत हाल’ के साथ लाज़िमी तौर पर वाबस्ता है। ‘वजूदी तजुर्बा’ दुख से कभी ख़ाली नहीं हो सकता। यह ‘दुख’ बुद्ध के दुख से इन माएनों में अलग हो जाता है कि यह एक एहसास-ए-जुर्म (Guilt) भी पैदा करता है। उजाले दीप में ‘दुख’ और एहसास-ए-जुर्म का यह वजूदी रिश्ता बहुत खुलकर सामने आया है।
वजूदी तजुर्बे में ‘मौत का शऊर’ भी हर हाल में शामिल रहता है। हमारी तमाम ज़िंदगी मौत के इस शऊर की रहनुमाई में ही ख़ुद को ढालती और अपनी शक्ल तब्दील करती रहती है। इंसान को यह तमाम तजुर्बे एक किस्म की थकन, गिरावट और उदासी (depression) से जोड़े रखते हैं। कार्ल यास्पर्स ने इसे (Feeling of Foundering) का नाम दिया है। यहाँ मैं वाज़ेह करना चाहूँगा कि इंसान का मतलब यहाँ ‘जदीद इंसान’ (आधुनिक मनुष्य) है, जिसकी हैसियत पुराने इंसान से अलग है। टी.एस. एलियट ने बीसवीं सदी की दूसरी दहाई में जिस Dissociation of Sensibility यानी होशमंदी के कट जाने की बात की थी, और जहाँ से अदब में मॉडर्निज़्म की बात शुरू हुई थी, वहीं से वजूदियत के रुझान के बीज भी पड़ना शुरू हो गए थे। यह रुझान पहली और दूसरी जंग अज़ीम के दरमियान अपने उरूज को पहुँच गया था और जिसके पैरोकारों में कार्ल यास्पर्स, हाइडेगर, ज़्यां पॉल सार्त्र, मार्टिन बूबेर और किसी हद तक अल्बेयर कामू भी शामिल थे (अल्बेयर कामू ने ख़ुद को कभी वजूदियतपसंद कहना पसंद नहीं किया, हालाँकि अगर वह वजूदियत पसंद नहीं थे तो फिर क्या थे? यह मुझे समझ में आज तक नहीं आया। क्यों कि कामू जिस Absurd की बात करते हैं, वह वजूदियत से बिल्कुल अलग नहीं है)। दिनेश श्रीनेत की कहानियों में जगह-जगह इस Absurd की झलकियाँ नज़र आती हैं। कहानी ‘उड़न खटोला’ में ख़्वाब, दुख, यादें और मौत मिलकर जिस बेमानीयत (Absurd) की रचना करते हैं, वह कहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ‘वहाँ मैं ख़ुद से भी मिलूँगा’ जैसा कहानी का आख़िरी जुमला एक वसीअ ख़्वाब की Absurd कामना के सिवा कुछ नहीं।
‘विज्ञापन वाली लड़की’ दिनेश की शायद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली कहानी है। इस कहानी का उर्दू में भी तर्जुमा किया गया। पाकिस्तान से आसिफ़ फ़र्रुखी के रसाले ‘दुनियाज़ाद’ में जब यह शाया हुई थी तो इसकी बड़ी धूम मची थी। यह कहानी ख़्वाब, सर्रियलिज्म, मौत, वाहमा (illusion) और हक़ीक़त की सरहदों को मिटाकर रख देती है। इसका narrative इतना जानदार है कि हिंदी-उर्दू कहानी में इतने पावरफ़ुल narrative की मिसाल कम ही मिलेगी।
यह कहानी Nothingness के वजूदियत के दिनों को दर्शाती है। न सिर्फ़ यह बल्कि उनकी कहानी ‘मात्र्योश्का’ भी। यहाँ अगर मौत नाम की कोई चीज़ ही न होती तो बुनियादी वजूद (Being) की तरफ़ हमारा ध्यान कभी न जाता। मगर चूँकि दुनिया फानी है और मौत हर तरफ़ से हमारे वजूद को घेरे हुए है, इसलिए इस अदम वजूद (Nothingness) का हमें वाज़ेह इदराक हो जाता है। बक़ौल हाइडेगर यह Nothingness हमारे वजूद (Existence) की नफी नहीं है, बल्कि इस Nothingness में इंसानी बुनियादी वजूद (Being), जो एक भेद या रहस्य है, इस रहस्य को समझने के लिए एक खिड़की भी खुलती है।
मेरा ख़याल है कि दिनेश श्रीनेत की यह पाँच कहानियाँ मिलकर इंसानी वजूद के राज़ या भेद को समझने के लिए एक खिड़की खोलती हैं। यह कहानियाँ एक तरह से अपने वजूद के पर्दे उठाए जाने की सरसराहट या एक पुकार हैं। इसी लिए दिनेश की तहरीरों में ज़िंदगी का अलमिया एहसास पाया जाता है। यह अलमिया एहसास ही उनकी वजूदियत की फ़िक्र की असास है, जिसके दायरे में इन कहानियों के किरदार अपनी नफ़्सियाती, जज़्बाती और तहज़ीबी कश्मकश के साथ अपना रोल निभाते हैं। हर किरदार मौत के शऊर को साथ लिए चलता है, क्योंकि मौत का शऊर ही इंसान के वजूद का बुनियादी उनसुर है और इसी उनसुर (तत्व) की बिना पर इंसान का वजूद हैवान से अलग होकर अपनी शनाख़्त बनाने में कामयाब हो पाता है।
दिनेश को कहानी कहने (storytelling) के फ़न पर मुकम्मल गिरफ़्त हासिल है। वह इस फ़न की तमाम बारीकियों और तकनीकों से वाक़िफ़ हैं। उन्होंने सर्रियलिज्म, सिनेमेटिक और फ़्लैशबैक तकनीकों को बहुत ख़ूबी के साथ इस्तेमाल किया है। ‘उजाले के दीप’ और ‘नीलोफ़र’ फ़्लैशबैक और सिनेमेटिक तकनीक की उम्दा मिसालें हैं। और इस पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि दिनेश सिनेमा के फ़न से बख़ूबी वाक़िफ़ हैं और अक्सर फ़िल्मों पर लिखते भी रहते हैं।
दिनेश की ज़बान या भाषा के बारे में पहले बात हो चुकी है। यहाँ इतना और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ऐसे कहानीकार कम हैं जो भाषा की ख़ामोशी को उसका जायज़ मक़ाम दे सकें। तनकीद निगारों ने ज़्यादातर बने-बनाए अदबी और जमलियाती (Aesthetic) तकाज़ों से ही सरोकार रखा और इसमें भी घिसी-पिटी बातों को ही दोहराते रहे या फिर सियासी, समाजी और माशी वाबस्तगी और शऊर की डफली पीटी जाती रही। एडवर्ड सईद ने कहा था कि हर फ़नकाराना चीज़ को सियासी रंग मत दीजिए, वरना आख़िर में कोई भी एहतेजाज बाक़ी नहीं रहेगा। बेहतर होगा कि आर्ट को सियासत पर एक मुक़दमे की तरह सोचा जाए।
ज़ाहिर है कि आर्ट की अपनी शर्तें होती हैं। अगर वह सियासी रंग इख़्तियार कर लेगा तो अपनी शर्तों को खो देगा और महज़ एक नारा या रिपोर्टिंग बन कर रह जाएगा। दिनेश इस नुक़्ते को जानते हैं और अपनी कहानी को हर किस्म के चालू और फ़ैशनेबल रुझान से साफ़ बचा ले जाते हैं। वह कहानीकार हैं और वही बने रहना चाहते हैं। वह ‘वाक़िया’ या घटना की तलाश में इतना परेशान होना पसंद नहीं करते कि उनकी पहचान फ़िक्शन लिखने वाले से ज़्यादा तारीख़दाँ की होकर रह जाए। हाँ अगर किसी को दिनेश के सियासी या समाजी शऊर से दिलचस्पी हो तो उसको उनके लेख पढ़ने चाहिए और उनकी अमली ज़िंदगी या पेशेवर ज़िंदगी के बारे में ज़रूर कुछ जानना चाहिए। उनकी कहानियों से सरसरी तौर पर यह उम्मीद लगाना बेकार होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि अदब, भले ही अपने अहद के ज़मीर की आवाज़ होता है, मगर ज़िंदगी के उसूल और साहित्य या कला के उसूल एक जैसे नहीं होते। वह अलग-अलग होते हैं। इसलिए अदब सिर्फ़ दुनिया की नुमाइंदगी ही नहीं करता। वह एक नई दुनिया की तश्कील (निर्माण) भी करता है।
दिनेश श्रीनेत की अनोखी कहानियों का यह संग्रह हिंदी-कथा कहने के क्षेत्र में एक बड़े सरमाए के इज़ाफे की हैसियत रखता है।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
12 जून 2025
‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही’
‘बॉर्डर 2’ का विचार सुनते ही जो सबसे पहला दृश्य मन में कौंधा, वह बालकनी में खड़े होकर पिता का कहना था—‘अब सनी देओल में वो बात नहीं रही।’ इस वाक्य में सिर्फ़ एक अभिनेता का अवसान नहीं था, एक पूरे युग क
29 जून 2025
‘बिंदुघाटी’ पढ़ते तो पूछते न फिरते : कौन, क्यों, कहाँ?
• उस लड़की की छवि हमेशा के लिए स्टीफ़न की आत्मा में बस गई, और फिर उस आनंद में डूबा हुआ पवित्र मौन किसी भी शब्द से नहीं टूटा... आप सोच रहे होंगे कि यहाँ किसी आशिक़ की किसी माशूक़ के लिए मक़बूलियत की बा
14 जून 2025
बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल!
‘बेवफ़ा सोनम बनी क़ातिल’—यह नब्बे के दशक में किसी पल्प साहित्य के बेस्टसेलर का शीर्षक हो सकता था। रेलवे स्टेशन के बुक स्टाल्स से लेकर ‘सरस सलिल’ के कॉलमों में इसकी धूम मची होती। इसका प्रीक्वल और सीक्वल
10 जून 2025
‘जब सोशल मीडिया नहीं था, हिंदी कविता अधिक ब्राह्मण थी’
वर्ष 2018 में ‘सदानीरा’ पर आपकी कविता-पंक्ति पढ़ी थी—‘यह कवियों के काम पर लौटने का समय है’। इस बीच आप फ़्रांस से लौटकर आ गए। इस लौटने में काम पर कितना लौटे आप? 2018 में जब यह कविता-पंक्ति संभव हुई
20 जून 2025
8/4 बैंक रोड, इलाहाबाद : फ़िराक़-परस्तों का तीर्थ
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एम.ए. में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी मेरे मित्र बन गए। मैं उनसे उम्र में छोटा था, लेकिन काव्य हमारे मध्य की सारी सीमाओं पर हावी था। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। उनका नाम वीरेंद्र