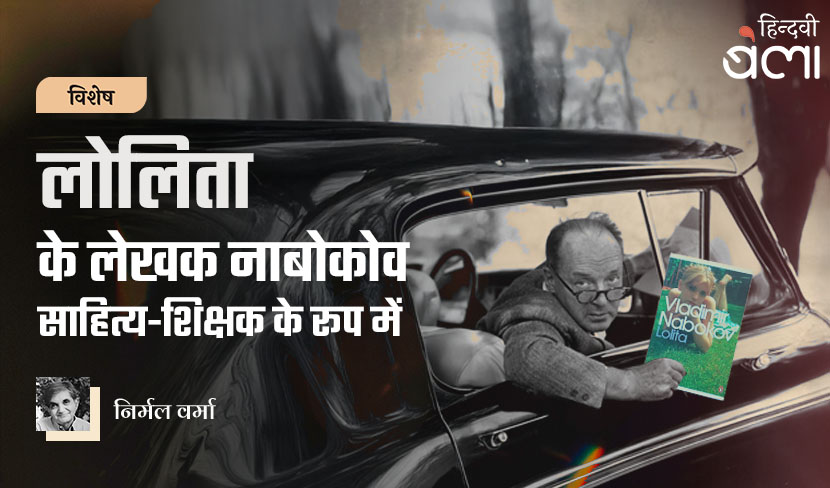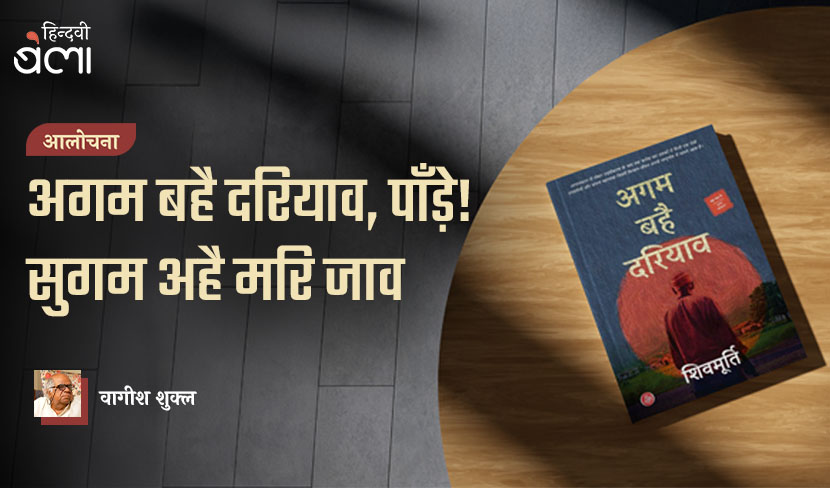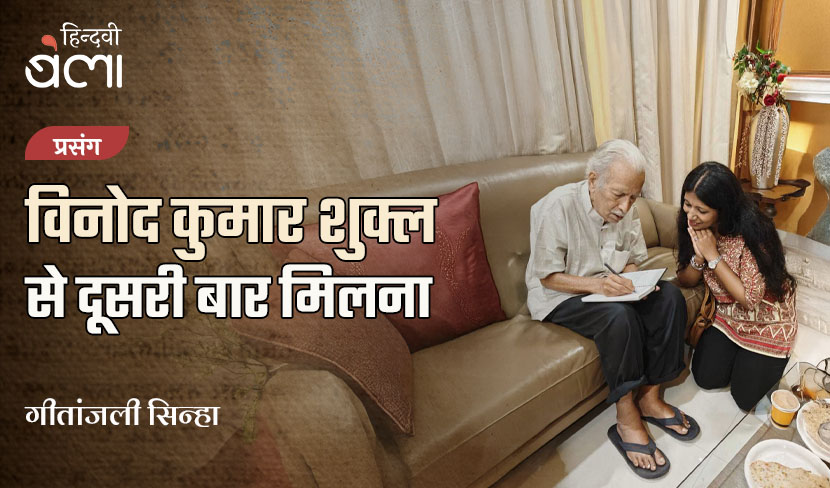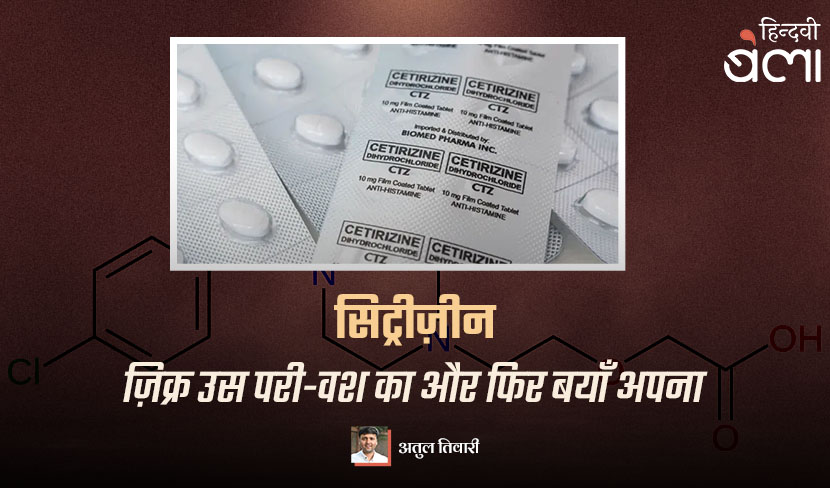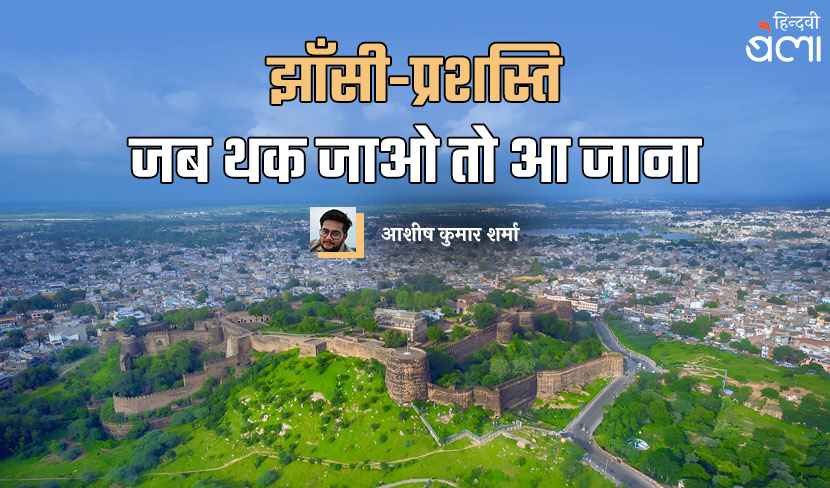इक़बाल : विरोधाभासों से भरा एक राजनीतिज्ञ
 हिन्दवी डेस्क
09 नवम्बर 2025
हिन्दवी डेस्क
09 नवम्बर 2025

इक़बाल एक महान् कवि थे, इक़बाल एक महान् दार्शनिक थे, इक़बाल एक महान् चिंतक थे, इक़बाल एक महान् मुस्लिम थे आदि-आदि। इक़बाल के बारे में हम ज़्यादातर यही सुनते आए हैं। इक़बाल जो भी हैं महान् हैं। महान् लोगों में विरोधाभास होते हैं। लेकिन इक़बाल विरोधाभासों से भरे हुए तो हैं, लेकिन महान् क्यों हैं और किस लिए हैं—ये तथ्यों से परे है। साम्यवादी हों या राष्ट्रवादी या फिर सांप्रदायिक, तीनों ही इक़बाल को अपनाने की कोशिश करते हैं। सभी को इक़बाल के यहाँ कुछ न कुछ मिल जाता है। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है! मुस्लिम आख्यान-निर्माताओं ने शुरू से ही जिन व्यक्तित्वों को आदर्श के रूप में अपनी क़ौम के सामने पेश किया, उन सभी को एक ऐसे पायदान पर बिठा दिया कि जहाँ से सिर्फ़ उनका प्रशस्तिगान ही संभव था। इस प्रकार के प्रस्तुतिकरण ने इन लोगों में निहित अंतर्विरोधों पर न तो ख़ुद ही बात की और न ही किसी और को करने दी। उसी के कारण सही को सही और ग़लत को ग़लत कहकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की यात्रा को प्रशस्त करने के स्थान पर असहज करने वाले तथ्यों को छुपाकर इन आख्यान-निर्माताओं ने उसके अवरोधक के रूप में काम किया है। व्यक्ति कोई भी हो आलोचना से परे नहीं है और आलोचनात्मक मूल्यांकन ही मुस्लिम जन मानस को सही आदर्शो की ओर बढ़ाकर उनकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा और अन्य भारतीयों के साथ उनकी स्थिति भी बेहतर करेगा। कविता और भाषणों एवं व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना इक़बाल का यह आलोचनात्मक मूल्यांकन इसी कड़ी का एक अंश है।
इक़बाल और विरोधाभास
परवेज़ हुडभॉय का मानना है कि सभी को अपने मतलब का कुछ न कुछ अंश इक़बाल की शाइरी में मिल ही जाता है। एक सैद्धांतिक और स्पष्ट विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ ऐसा होना संभव नहीं मालूम होता है, अर्थात् यह बात साफ़ है कि इक़बाल अलग-अलग भाषाओं में अपने अलग-अलग रूप, पाठक वर्ग के सामने रखते हैं। तहरीक-ए-पाकिस्तान की स्थापना करने वाले पाकिस्तानी धर्मगुरु ख़ादिम हुसैन रिज़वी इक़बाल की शाइरी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ और ईशनिंदा क़ानून के समर्थन में जुलूस निकालते हैं तो वहीं पाकिस्तान का एक प्रगतिशील वर्ग इक़बाल के ज़रिए आधुनिक शिक्षा हेतु लोगों को प्रोत्साहित करता है। इक़बाल ने महिलाओं को बीबी फ़ातिमा (हज़रत मोहम्मद की बेटी और हज़रत अली की बीवी) की मिसाल देकर उन के जैसा बनने के लिए कहा, किंतु हज़रत ख़दीजा का उदाहरण नहीं दिया।
विरोधाभास और इक़बाल का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। जहाँ अपने जीवन के पहले चरण में वह अंजुमन-ए-हिमायत-ए-इस्लाम के नियमित सदस्य थे। वहीं साथ-साथ हिन्दू-मुस्लिम एकता की भी बात करते थे। (पृ.107)
उनके अनुसार धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध था, लिहाज़ा मुसलमानों को इस्लाम द्वारा निर्देशित मूल्यों पर चलने वाले राज्य में ही रहना चाहिए। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन सब बातों को विस्तारपूर्वक लिखने के लिए उन्होंने उर्दू नहीं वरन् अँग्रेज़ी भाषा को चुना। (पृ.108)
भाषा और उसके खेल को इक़बाल बहुत अच्छे से समझते थे और इसीलिए उनके एक ही दौर की लेखनी में मौजूद विचारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के अनुसार परिवर्तन साफ़ दिखता है। अभिजात्य मानसिकता उनके अंदर किस क़दर रची-बसी थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने लिखा है कि मेरे ख़्याल इतने ऊँचे हैं कि केवल फ़ारसी ही उसके लिए उपयुक्त है। (पृ. xiii, ज़फ़र अंजुम)
राजकुमार त्रिवेदी अपनी पुस्तक ‘द क्रिटिकल ट्राइएंगल’ में लिखते हैं कि 1910 के बाद पैन-इस्लामिक अवधारणा इतनी गहरी पैठ कर चुकी थीं कि राष्ट्रवादी कवि माने जाने वाले इक़बाल भी इस वक़्त तक इसी पहचान का आलिंगन कर चुके थे। मोहम्मद अली (1878- 1931) ने तो उन्हें भारत में मुस्लिम चेतना के जागरण का कवि कहा है। (पृ. 133)
“इक़बाल के विचार यूरोप में बिल्कुल बदल गए थे, वह देशभक्त की बजाय पैन इस्लामिस्ट (विश्व इस्लामवादी) हो गए थे।” (फ़िराक़, 234)
इस बात को और अधिक बल मोईन शाकिर के इस कथन से मिलता है कि “इक़बाल का दर्शन मात्र भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक विचार पुष्ट करने में प्रभावी था।” (पृ. 95)
उनका विरोधाभास और भी अधिक तब स्पष्ट होता है जब पैन-इस्लाम की पहचान को ख़ुशी से अपना लेने वाले इक़बाल ‘ख़िलाफ़त आंदोलन’ पर मूक दर्शक बने रहे और इससे भी आश्चर्यजनक बात यह कि तुर्की में ख़िलाफ़त की संस्था के उन्मूलन को सराहा भी। (राजकुमार त्रिवेदी, ‘द क्रिटिकल ट्राइएंगल’, पृ.201- 202)
इस वक़्त पर कमाल अतातुर्क उर्फ मुस्तफ़ा कमाल पाशा की तारीफ़ों के पुल बाँधने वाले इक़बाल एक वक़्त पर आकर कहते हैं कि एशिया की आत्मा अतातुर्क के द्वारा बनाए गए बंधन में फँसी हुई है। (राजमोहन गांधी, ‘अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड’, पृ.47-53)
इक़बाल ने उस समय भी ख़ामोशी अपनाए रखी जब साम्राज्यवाद का विरोध अपने चरम पर था और भारत में जलियाँवाला बाग़ जैसी एक नृशंस घटना हो चुकी थी। इस घटना से जन भावना इतने आवेग पर थी कि इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रवींद्रनाथ टैगोर ने जलियाँवाला बाग़ नरसंहार के विरोध में अपना नाइटहुड (सर की उपाधि) लौटा दिया था। उस वक़्त पर इक़बाल की ओर से विरोध का कोई स्वर आना तो दूर रहा, उल्टा उनका यह आग्रह रहा कि उन्हें सर मोहम्मद इक़बाल कहकर संबोधित किया जाए। (त्रिपुर्दमन सिंह एवं आदिल हुसैन, ‘नेहरू: द डिबेट्स दैट शेप्ड इंडिया’, पृ.4)
उनके दार्शनिक होने को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, किंतु सच्चाई यह है कि 1907 में ‘डेवलपमेंट ऑफ़ मेटाफ़िज़िक्स इन पर्शिया’ पर शोधकार्य करके जब इक़बाल ने म्यूनिख विश्वविद्यालय को अपना शोधकार्य जमा किया तो उसे दर्शनशास्र नहीं वरन् भाषाशास्त्र की डिग्री के लिए उपयुक्त माना गया। (परवेज़ हुडभॉय, ‘पाकिस्तान : ओरिजन्स, आइडेंटिटी ऐंड प्रेजेंट’, पृ.107)
इक़बाल ने स्वयं कहा है कि मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो दर्शनशास्र से ही घृणा है। जो बातें मैं करता हूँ उनमें दार्शनिकों की भी रुचि होती है, किंतु मेरे लिए वे सभी बातें आत्मानुभव से पनपी हुई होती हैं किसी दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित नहीं। (मोईन शाकिर, ‘फ्रॉम ख़िलाफ़त टू पार्टीशन’, पृ.95)
यहाँ तक कि इक़बाल ने तो सूफ़ियों तक का यह कहकर विरोध किया कि वह लोगों को एब्सट्रेक्ट के अतिरिक्त और कुछ देने में असमर्थ हैं।
इक़बाल द्वारा लिखी कुछ नज़्में जैसे ‘कार्ल मार्क्स की आवाज़’, ‘बोलशेविक रूस’, ‘लेनिन ख़ुदा के हुज़ूर में’, ‘सरमाया ओ मेहनत’ आदि उन्हें साम्यवाद के हिमायती के रूप में पेश करती हैं और यही बात एक भारतीय कम्युनिस्ट शमसुद्दीन हसन ने ‘ज़मींदार अख़बार’ में भी लिखी है। (परवेज़ हुडभॉय, ‘पाकिस्तान : ओरिजन्स, आइडेंटिटी ऐंड प्रेजेंट’, पृ.109)
हक़ीक़त यह है कि फ़िराक़ गोरखपुरी ने इक़बाल की कम्युनिस्ट विचारधारा की पोल खोल दी है। उनके अनुसार इक़बाल साम्यवाद से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। “धर्म निरपेक्षता से उन्हें ऐसी चिढ़ है कि वह धर्म-निरपेक्ष मज़दूर राज्य की भी भर्त्सना कर देते हैं। मार्क्सवाद के भौतिकवादी दृष्टिकोण के वह दुश्मन थे।” (फ़िराक़, 238)
इक़बाल और राष्ट्रवाद
इक़बाल के अनुसार पूँजीवाद के कारण ही राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था और राष्ट्रवाद एवं देश-प्रेम में बहुत अंतर है। जहाँ वह ख़ुद को देश-प्रेम का समर्थक बताते हैं, वहीं उनका मानना था कि राष्ट्रवाद इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। (मोईन शाकिर ‘फ्रॉम ख़िलाफ़त टू पार्टीशन’, पृ.99)
जवाहरलाल नेहरू के साथ कोलकाता के ‘मॉडर्न रिव्यू’ में कादियानियों को लेकर हुई बहस में इक़बाल का इस्लाम की श्रेष्ठता में विश्वास और धर्म के आधार पर राष्ट्र-निर्माण का समर्थन खुलकर सामने आता है। वह कहते हैं कि तुर्की, ईरान, इराक़ एवं अन्य मुस्लिम देशों में राष्ट्रवाद कभी कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेगा, परंतु भारत में वह राष्ट्रवाद के समर्थक मात्र इसलिए नहीं होना चाहते थे क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक समुदाय मुसलमान नहीं था। (शामलू द्वारा संपादित, ‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ.142)
बहुसंख्यक आबादी के साथ मिलकर रहने को इक़बाल ने अल्पसंख्यकों के अस्तित्व पर ख़तरा बताया है और कहा है कि ऐसा करने पर वह अपना अस्तित्व खो देंगे। (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ.210)
इक़बाल ने यह भी कहा कि यदि विभिन्न संप्रदायों के मिलाप को राष्ट्रीयता समझा जाता है तो मैं यह कहने में कोई संकोच नहीं महसूस करता कि मैं राष्ट्र-विरोधी हूँ। (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ.193)
भारत के विषय में इक़बाल कहते हैं कि भारत की समस्या के दो ही विकल्प हैं, जिनमें से किसी एक को अपनाकर ही कोई समाधान हो सकता है। पहला विकल्प है पूर्व (भारत) में सदा के लिए एक ब्रिटिश एजेंट तैनात रहे और दूसरा विकल्प है कि धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आधार पर देश का पुनर्गठन हो। (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ.195)
मौलाना हुसैन अहमद मदनी द्वारा दिए गए मुत्ताहिदा क़ौमियत के सिद्धांत का घोर विरोध करते हुए कहा कि भौगोलिक सीमा पर आधारित राष्ट्रवाद आधुनिक पश्चिमी सभ्यता की देन है और इस्लाम के पूर्णतः विरुद्ध। (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ.204)
इक़बाल का मानना था कि आधुनिक राष्ट्रवाद अधार्मिकता को जन्म देगा और इस कारण मुसलमान अपने धर्म से हाथ धो बैठेंगे। यह आंकलन पूरी तरह ग़लत है क्योंकि हक़ीक़त यह है कि इक़बाल भारत के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को समझ ही नहीं सके थे। जैसा कि राजीव भार्गव बताते हैं अशोक से लेकर गांधी के वक़्त तक धर्म पर चर्चा और उसके प्रति सहिष्णुता भारतीयता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आधार थे। इक़बाल इस बात को समझने में असमर्थ थे, क्योंकि मुस्लिम शासकों से पहले के भारत के साथ इक़बाल ने कभी कोई संवाद स्थापित करने का प्रयास ही नहीं किया। “धर्म निरपेक्षता से उन्हें ऐसी चिढ़ है कि वह धर्म-निरपेक्ष मज़दूर राज्य की भी भर्त्सना कर देते हैं। मार्क्सवाद के भौतिकवादी दृष्टिकोण के वह दुश्मन थे।” (फ़िराक़, 238)
इक़बाल जातीय एकरूपता के बहुत बड़े समर्थक थे, यही कारण है कि वो “पंजाब राज्य से अंबाला को बाहर करने के लिए तैयार थे।” (वेंकट धूलीपला, ‘क्रिएटिंग ए न्यू मदीना’, पृ.144)
बावजूद अपनी ग़लत धारणा के उन्होंने अपनी कमी को तो छिपाया ही पर साथ ही साथ नेहरू जैसे विद्वान पर उन्नीसवीं सदी के इस्लाम को न समझ पाने का आक्षेप भी लगाया। (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ.130)
इस बात को गहराई से देखने पर अंदाज़ा होता है कि दरअस्ल इक़बाल को उन्नीसवीं सदी के इस्लाम के विषय में जानकारी का अभाव था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं होगा, वह जमालुद्दीन अफ़ग़ानी (1838-1897), सर सैयद अहमद खान (1817-1898) और मुफ़्ती अलमारी जान को एक ही श्रेणी में रखते हुए, उन्हें अब्दुल वहाब (1703-1792) से प्रेरित नहीं बता सकता। उनकी दृष्टि में एक और त्रुटि यह है कि उन्होंने वहाबियों को इज्तिहाद (दलील की रौशनी में स्वयं आंकलन करने) का पैरोकार बताया है (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ. 133) किंतु शाह वलीउल्ला (1703-1762) ने उलेमाओं और आलिमों को ही इज्तिहाद के योग्य माना है।
‘यादों की दुनिया’ पुस्तक में यूसुफ़ हुसैन ख़ान ने बताया है, जब वह वर्ष 1937 में इक़बाल से मिले, तब तक उन्होंने एक पृथक राष्ट्र का विचार त्यागा नहीं था। वह इस बात को लेकर चिंतित थे कि यदि भारतीय मुसलमान अपना अलग राष्ट्र नहीं हासिल करेंगे, तब तक उसके धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं हो पाएगी। (पृ.194- 95)
इक़बाल को राष्ट्रवादी बताने वाले लोगों को ऐसा करने के लिए भीमराव आंबेडकर के विद्वतापूर्ण कथन के विरुद्ध जाना पड़ेगा। आंबेडकर कहते हैं, “इक़बाल किसी भी ग़ैर-मुस्लिम देश के मुसलमानों में मातृभूमि के प्रति प्रेम से उपजे राष्ट्रीय भाव का पुरज़ोर विरोध करते हैं। (आंबेडकर, ‘पाकिस्तान अथवा भारत विभाजन’, पृ.332)
इक़बाल की कादियानियों को लेकर राय (और मुस्लिम देश में अल्पसंख्यकों पर भी)
“इक़बाल ने इस बात को स्वीकार किया कि इस्लाम इस बात पर ज़ोर देता है कि दुनिया के अलग-अलग समुदायों को एक ही समुदाय में समाहित किया जाए। इसलिए कोई भी ऐसी आवाज़ जो इस्लाम की एकरूपता और मज़बूती पर प्रहार करेगी उसे सहा नहीं जाएगा। बहाईवाद को क़ादियानियों से बेहतर बताया। इसका कारण यह है कि बहाईवाद पूरी तरह इस्लाम से भिन्नता दर्शाता है, जबकि कादियानी कुछ इस्लामी तत्व रखते हुए भी ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं जो इस्लाम के मूल के विरुद्ध है।” (शामलू द्वारा संपादित ‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ.94-95)
इक़बाल का मानना यह भी था, “भारत में उदारवाद की नीति के परिणाम बहुत घातक रहे हैं।” (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ. 97)
वह कहते हैं कि “सामुदायिक जीवन भी विघटनकारी ताक़तों से उतना ही प्रभावित होता है जितना निजी जीवन (व्यक्तिगत जीवन) आधुनिक उदारवादी सिद्धांतों के तहत धर्म को लेकर सभी प्रकार की आज़ादी मिलने से धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को बहुत नुक़सान पहुँचेगा।” (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ. 99)
इन सब दलीलों द्वारा उनकी माँग यह थी, “सरकार क़ादियानियों को एक अलग धार्मिक समुदाय घोषित कर दे।” (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ.100-101) इस पर सबसे अच्छी टिप्पणी है—“कभी-कभार इक़बाल को स्वयं भी समझ नहीं आता था कि वह कितनी विरोधाभासपूर्ण बात कर रहे होते थे। उदाहरणार्थ उन्होंने जब यह कहा कि अँग्रेज़ी सरकार को कादियानियों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, तब वह अपने ही धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे।” (त्रिपुर्दमन सिंह एवं अदील हुसैन, ‘Nehru : The Debates that define India’, p.9)
इक़बाल ने क़ादियानियों के अख़बार ‘लाईट’ में प्रकाशित दावे पर बात करते हुए कहा कि हालाँकि मैं मनुष्य की आध्यात्मिक कुव्वत पर भरोसा रखता हूँ, मगर यह नहीं मान सकता कि आध्यात्मिक व्यक्तित्व उस गणितीय समीकरण के तहत जन्म लेते हैं जैसा कि ‘लाइट’ में लिखा है। (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ.102)
सनराइज अख़बार ने कहा कि इक़बाल में निरंतरता की कमी है, क्योंकि आज जहाँ वह इस आंदोलन के समर्थक थे, वहीं आज उस पर बहुत कठोर प्रहार कर रहे हैं। इस पर इक़बाल ने कहा कि पच्चीस वर्ष पहले मुझे इस आंदोलन से कुछ उम्मीद थी। उस वक़्त तो चिराग़ अली ने भी आंदोलन के संस्थापक के साथ मिलकर एक किताब ‘बराहीन-ए-अहमदिया’ लिखी। (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृष्ठ 103)
“जब एक संस्कृति का पतन होता है तो उसके धार्मिक अनुभवों के प्रकार तथा दार्शनिक चर्चाएँ संकुचित होने लगती हैं।” (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ.106)
“स्टेट्समैन, 10 जून 1935 के लेख के जवाब में कहा कि सरकार को ख़ुद मुस्लिम पक्ष का ध्यान रखते हुए क़ादियानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए थी क्योंकि 1919 में सिखों के मामलें में ऐसा किया गया था, जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें हिंदू धर्म में ही माना था।” (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ.107)
इक़बाल ने कहा कि एक ईश्वर में यक़ीन, पैगंबरों में विश्वास और यह भरोसा कि हज़रत मोहम्मद ही अंतिम पैगंबर हैं—मुसलमानों के सबसे ख़ास चरित्र हैं जिसमें अंतिम तो मुसलमानों और ग़ैर-मुसलमानों के बीच भेद स्पष्ट करने का सबसे बड़ा परिचायक है। इक़बाल ने क़ादियानियों की ब्रह्म समाज से तुलना की और कहा दोनों ही इस्लाम के तहत नहीं आते क्योंकि वे हज़रत मोहम्मद को आख़िरी पैगंबर नहीं मानते।” (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ.108)
“क़ादियानियों के पास दो ही रास्ते मौजूद हैं—या तो ईरान के बहाईयों का अनुकरण करें या इस्लामी विचार को स्वीकार कर लें।” (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, 108-109)
“क़ादियानियों के संस्थापक ने इस्लामिक समुदाय को फटे दूध की संज्ञा दी थी। कादियानियों को ताज़ा दूध की संज्ञा दी और कहा हम इनके साथ न मिलें। उन्होंने ख़ुद को अहमदिया कहा, वे लोग बाजमात-नमाज़ में शामिल नहीं होते थे।” (‘स्पीचिज़ ऐंड स्टेटमेंट्स ऑफ़ इक़बाल’, पृ.109)
इक़बाल ने पाकिस्तान निर्माण के विचार की नींव रखी इस बात को वेंकट धूलीपला और आंबेडकर दोनों ही पुरज़ोर तौर पर सामने लाते हैं। (वेंकट धूलीपला, ‘क्रिएटिंग ए न्यू मदीना’, पृ.128)
मख़फ़ी के छद्म नाम से सन् 1925 के आस-पास ‘रंगीला रसूल’ नामक पुस्तक लिखी गई, जिसे महाशय राजपाल ने प्रकाशित किया था। ज़्यादातर संभावना थी कि “यह पुस्तक डी ए वी कॉलेज के प्रोफ़ेसर चंपापति द्वारा लिखी गई थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ‘प्रताप’ के संपादक कृष्ण इसके पीछे थे। जून 1927 में राजपाल को लाहौर हाईकोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया।” इसके बावजूद पंजाब के मुस्लिम भरी असंतोष पाले रहे और उनकी इस भावना को मूर्त रूप दिया इल्मदीन नामक एक व्यक्ति ने जिसने राजपाल की हत्या कर दी। उसके जनाज़े में न सिर्फ़ इक़बाल शामिल हुए बल्कि सारे इंतज़ाम बढ़-चढ़ कर कराए। (जाफ़र बलोच, ‘अल्लामा इक़बाल और मौलाना ज़फ़र अली खान’, पृ. 35-40)
यही नहीं उन्होंने इल्मदीन को शहीद क़रार देते हुए उसकी प्रशंसा में यह कहा कि इस्लाम के इस मतवाले ने वह कर दिखाया जो यह कलमकार (इक़बाल) नहीं कर पाया, यानी हज़रत मोहम्मद की शान में गुस्ताख़ी करने वाले को मार गिराया (इश्तियाक़ हुसैन, ‘जिन्ना : हिज़ सक्सेसेज़, फ़ेल्योर्स ऐंड रोल इन हिस्ट्री’, पृ.475)
मोहम्मद मुजीब का भी मानना यह है कि इक़बाल मानव और वैश्विकता के कल्याण की बात तो करते हैं, परंतु मानव का अर्थ उनके लिए मुसलमान और विश्व का अर्थ इस्लामी दुनिया हो जाता था। (राजमोहन गांधी, ‘अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड’, पृ.152)
इक़बाल के तमाम विरोधाभासी पहलुओं के कारण विभिन्न विचारधारा के समर्थकों द्वारा अपने लिए उपयोग के कारण ही इक़बाल के अतिया फ़ैज़ी को लिखे ख़त में की गई भविष्यवाणी सही साबित होती दिखती है। इक़बाल ने यह अंदेशा जताया था कि आगे चलकर लोग उनको अवश्य पूजेंगे और ऐसा ही अब तक होता रहा है। इसी कारण इक़बाल को उनकी समग्रता में तमाम विरोधाभासों के साथ देखना आवश्यक है, ताकि उनको लेकर कोई भी अतिवादी दृष्टि न बने और इतिहास उनका सही मूल्यांकन कर सके।
•••
लेखक : भावुक (शोधार्थी, इतिहास विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी) और विष्णु प्रभाकर उपाध्याय (शोधार्थी, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी) | इक़बाल को यहाँ पढ़ सकते हैं : इक़बाल
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
25 अक्तूबर 2025
लोलिता के लेखक नाबोकोव साहित्य-शिक्षक के रूप में
हमारे यहाँ अनेक लेखक हैं, जो अध्यापन करते हैं। अनेक ऐसे छात्र होंगे, जिन्होंने क्लास में बैठकर उनके लेक्चरों के नोट्स लिए होंगे। परीक्षोपयोगी महत्त्व तो उनका अवश्य होगा—किंतु वह तो उन शिक्षकों का भी
06 अक्तूबर 2025
अगम बहै दरियाव, पाँड़े! सुगम अहै मरि जाव
एक पहलवान कुछ न समझते हुए भी पाँड़े बाबा का मुँह ताकने लगे तो उन्होंने समझाया : अपने धर्म की व्यवस्था के अनुसार मरने के तेरह दिन बाद तक, जब तक तेरही नहीं हो जाती, जीव मुक्त रहता है। फिर कहीं न
27 अक्तूबर 2025
विनोद कुमार शुक्ल से दूसरी बार मिलना
दादा (विनोद कुमार शुक्ल) से दुबारा मिलना ऐसा है, जैसे किसी राह भूले पंछी का उस विशाल बरगद के पेड़ पर वापस लौट आना—जिसकी डालियों पर फुदक-फुदक कर उसने उड़ना सीखा था। विकुशु को अपने सामने देखना जादू है।
31 अक्तूबर 2025
सिट्रीज़ीन : ज़िक्र उस परी-वश का और फिर बयाँ अपना
सिट्रीज़ीन—वह ज्ञान के युग में विचारों की तरह अराजक नहीं है, बल्कि वह विचारों को क्षीण करती है। वह उदास और अनमना कर राह भुला देती है। उसकी अंतर्वस्तु में आदमी को सुस्त और खिन्न करने तत्त्व हैं। उसके स
18 अक्तूबर 2025
झाँसी-प्रशस्ति : जब थक जाओ तो आ जाना
मेरा जन्म झाँसी में हुआ। लोग जन्मभूमि को बहुत मानते हैं। संस्कृति हमें यही सिखाती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, इस बात को बचपन से ही रटाया जाता है। पर क्या जन्म होने मात्र से कोई शहर अपना ह