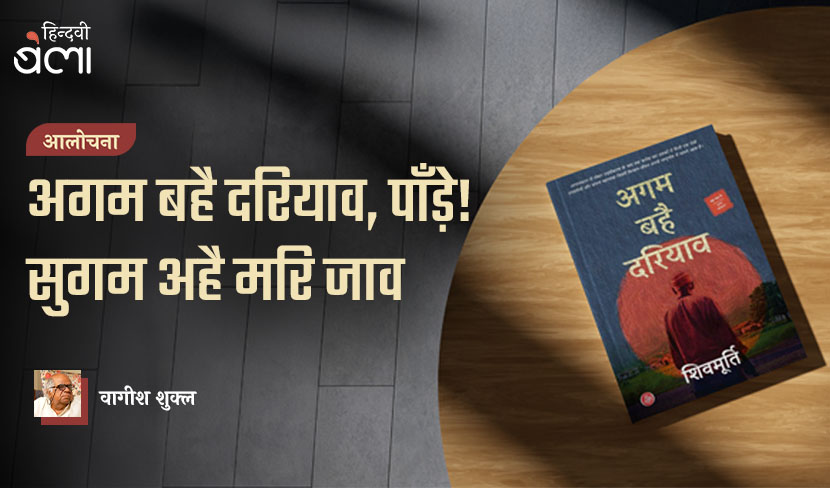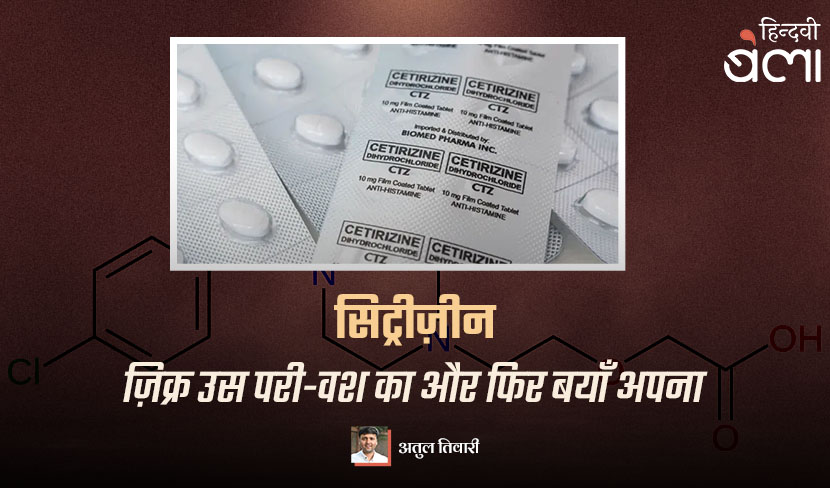आम की बेला
 आदित्य विक्रम
01 जुलाई 2025
आदित्य विक्रम
01 जुलाई 2025

मिरा वक़्त मुझ से बिछड़ गया मिरा रंग-रूप बिगड़ गया
जो ख़िज़ाँ से बाग़ उजड़ गया मैं उसी की फ़स्ल-ए-बहार हूँ
मुज़्तर ख़ैराबादी
ज़्यादा नहीं बीस बरस पहले तक, गाँवों में बाग़ों का अस्तित्व बचा हुआ था। हिंदी-कवि राजेश जोशी अपनी कविता ‘संयुक्त परिवार’ में कहते हैं—
टूटने की इस प्रक्रिया में क्या-क्या टूटा है
कोई नहीं सोचता
यह टूटना जिसे अवध में अलगौझी भी कहते हैं, वह तेज़ी से होना शुरू हो गया था— सामान्य अर्थों में बँटवारा; लेकिन यह बँटवारा बाग़ों के संदर्भ में उस तरह से नहीं दिखाई देता था जो घरों और सामानों के स्वामित्व में नज़र आता है। बाग़ किसी का भी हो, बच्चों और राहगीरों के लिए अपना ही होता था। दुकानें सिर्फ़ बाज़ारों में हुआ करती थी और बाज़ार—बाज़ार में। सड़कें बहुत दूर तक दोनों तरफ़ पेड़ों और खेतों से ही घिरी रहती थीं। छोटी दूरी के मुसाफ़िरों के लिए बाग़—मुसाफ़िरख़ाना का भी काम कर दिया करते थे। मुझे याद आता है कि गाँव के अधिकतर पुरुषों का जेठ और आषाढ़ महीना बाग़ों के सहारे ही कट जाया करता था। बाक़ी दिनों में बाग़ पूरे गाँव का सामुदायिक स्थल हुआ करती थी, उस समय सामुदायिक भवन कहीं-कहीं ही बने हुए थे।
वैसे एक और महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि हम पुरबियों के लिए बाग़ का मतलब आम के ढेर सारे पेड़ों का रिहाईश से थोड़ी ही दूर पर होना था। हाँ, आम के बीच- बीच में अगर जामुन भी हो तो क्या कहना। दरअस्ल दोनों का फल देने का समय आगे पीछे का ही था, तो एक ही मौसम दोनों के लिए बहार का था। जामुन के पेड़ के साथ एक दिक़्क़त थी कि उस पर बचकर चढ़ना होता था, बड़ी आरर होती है उसकी डाल। हर गाँव में कोई-न-कोई मिल जाता था, जो यह चिन्हाने के लिए होता कि जामुन से गिर कर एनकर हाथ टूट रहा।
बाग़ों के होने के महत्त्व का जो समय था, वह लंबी छुट्टियों के दिनों का भी समय था। तब ग्रीष्मावकाश की अवधि लंबी होती थी और ज़रूर होती थी| अब वह अवकाश टुकड़ों-टुकडों में होता है, शायद बाग़ों की आत्मा का यह बदला लेने का तरीक़ा हो। फिलहाल वे बाग़ अब ख़त्म होते जा रहे हैं। इन सब में एक और महत्त्वपूर्ण किरदार था बागों का। उस समय बाग़ मैरिज हॉल का भी किरदार निभाते थे। जनवासा बाग़ों में ही लगता था। मुझे याद है कि हमारे गाँव के इस्लाम भैया के पास डेरा होता था—जिसे शामियाना भी कहते हैं—जो शादियों में बुक किया जाता था। आज के समय के हिसाब से टेंट हाउस जैसा, अग़ल-बग़ल के अधिकतर गाँवों में उनका डेरा जाता था। यह डेरा या तो उस समय फ़सलों से ख़ाली हो चुके खेतों में लगता था या फिर उन्हीं बाग़ों में। डीजे का होना तो छोड़ दीजिए, लोगों की कल्पनाओं में भी इसका जन्म नहीं हुआ था। उन्हीं डेरों या तंबुओं के बॉस-बल्ली में भोपूँ वाले स्पीकर भी लग जाते थे, हालाँकि यह बहुत बाद की बात है। इस्लाम भैया को अग़ल-बग़ल के चार-पाँच कोस तक के सारे बाग़ों का भूगोल पता था।
बाग़ों में रहने का मौसम, जैसा मैंने बताया गर्मियों का है तो उस समय छात्र वृन्द सब ख़ाली हुआ करते थे। बाग़ उनके स्टेडियम बन जाते। खेल बहुत देशज थे और वह भी पानी और बोली की तरह कुछ-कुछ कोस पर अपने नियमों में बदलाव कर देते। वह कहावत है न ‘चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर वाणी’—इसी कहावत की तरह खेल के नियम भी बदलते थे। उस समय एक खेल हुआ करता था—बहुत याद करने पर नाम नहीं याद आ रहा—उसके दृश्य ज़रूर सामने आवा-जाही कर रहे हैं कि कैसे उसमें डंडा फेंका जाता, पेड़ पर चढ़ते, एक लड़का बोलता था, “बोल गोइयंवा पटरी सुतुर्रर्र” कुछ भाग-दौड़ होती थी। गाँव में चाचा को फोन किया तो पता चला उन खेलों के नाम चिल्होर, पटरी सुटुर्र थे। ये खेल वहाँ उपलब्ध संसाधनों में ही हो जाते थे, एक डंडा और कुछ ईटें। डंडा जो जानवर चराने वाले हर युवा का अस्त्र था और आसानी से उपलब्ध भी। यह बड़ी सहजता से खेला जाता था, जिसमें एक चोर बाक़ी सब साव थे। इस खेल मे लकड़ी के डंडे को लोग दूर फेंका करते थे। इसी फेंकने के दरमियान चोर को भी साव होने का एक छोटा-सा अवसर मिलता था, क्योंकि जैसे ही डंडा फेंका जाता था तो चोर बड़ी तेज़ी से फेंकने वाले को छूने का प्रयास करता था और वो झट से डंडे को दूर फेंककर ईंट पर अपना डंडा टिका देता था और साव बने रहने का ये एक सर्टिफ़िकेट था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था तो छुए जाने पर चोर बनने की बारी उसकी होती थी। गाय-भैसों को चराने लेकर जाने वाले बालकों के दिन-दुपहरिया का अस्थायी पता होते थे वे बाग़। बाग़ बड़ी सहूलत देती थे ताश खेलने वाले खिलाड़ियों को। एक तरह से गर्मी का महीना और बाग़ का माहौल ताश सीखने के लिए बिल्कुल माकूल था। उस पर फिर कभी तफ़्सील से बात होनी चाहिए।
आम के बाग़ों में आम थे। आज वाले ख़ास आम नहीं, वे आम दिनों वाले आम थे। उस समय हमें दो-तीन तरह के आमों का ही पता था। कुछ देशी, जो ज़्यादा मात्रा में थे और दूसरे विशिष्ट आमों में दशहरी और कलमी। कलमी और दशहरी आम बहुत मीठा होता है, इतना मीठा कि उसके कच्चेपन पर भी संकट था और पकने का मौक़ा किसी-किसी फल को ही मिल पाता था। लोगों का मानना था कि अगर पेड़ में रहे तो पकते-पकते कीड़े लग जाएँगे या फिर चिड़िया नहीं छोड़ेगी। हाँ कलमी से याद आया, ऐसे पेड़ो के बँटवारे में बड़ी समस्या होती थी। बाग़ों का बँटना मतलब पेड़ों का बँटना था। सामान्य पेड़ों का बँटवारा आराम से हो जाता, पर जिन पेड़ों के आम बहुत अच्छे होते थे, उनका बँटवारा न होकर सामूहिकता के साथ उसका संरक्षण होता था और फिर फलों का बँटवारा हो जाता था। हमारे दरवाज़े पर एक पेड़ कलमी आम का था तो उसके साथ भी यही सुलूक होता था। जो परिवार थोड़ा दूर रहता था, उसके मन में यह शंका हमेशा बनी रहती थी कि जो नजदीक है, वह फ़ायदा उठा रहा।
अब देशी आम को देखा जाए, तब तक बाज़ार में आमों की बहुत प्रजाति नहीं आई थी, पूरा गाँव समाज देशी आमों पर ही निर्भर था। गाँव में अभी तक बच्चों के नाम दिव्या और अक्षय रख जाना नहीं शुरू हुआ था। भगवान् के नाम की ही कॉपी चल रही थी, तो फिर आमों के कैसे नाम रखे जाते। देशी आमों के नामों में भी बहुत विविधता थी—नाम रखने का आधार तो सही-सही नहीं पता, पर लगता है कि उनके आकार, स्वाद और रूप के हिसाब से ही नाम रखा जाता रहा होगा। कुछ नाम याद आ रहें और उनके साथ एक कविता भी, ‘अवध और आम’ कवि केशव तिवारी की; जिसमें उन सब नामों का ज़िक्र है जिसे मैं कहना चाहता हूँ—
अवध और आम
अवध गमक रहा इन दिनों
दशहरी की महक से
दशहरी के कमज़ोर पड़ते ही
आएगा गदराया चौसा
पतले छिलके के रस से भरा
पूरे भादौं बहेगा इसका मीठा रस
अवध की नस-नस में
ये दुनिया में जहाँ भी पहुँचे हैं
पहुँचे हैं अपनी अवधी पहचान के साथ
कहीं-कहीं अभी भी खड़े हैं देशी दहक्खड़ आम
सेन्दुरिहा, खट्टुआ विसहरी, भदइयाँ की
अपनी जानी पहचानी खटास के साथ
सरपतिहा सेंवार से गुज़रते
छिल गए शरीर को सहलाते हवा
मिल जाएँगे इनकी छाँह में छहाते
गेहूँ कटाई के बीच इन्हीं से पीठ
टिकाए आम की चटनी रोटी खाते
मिल जाएँगे बिलासपुरिया कटइया मजूर
जेठ में आइए तो बस हवा में
एक ख़ास महक बता देगी
आप इस समय अवध में हैं
यह कविता आमों का काव्य शास्त्र है। सेंदुरहवा यह आम पीला और लाल दोनों रंग की आभा लिए हुए होता है और पूर्वांचल में सिंदूर पीला और लाल रंग का ख़ूब प्रचलन है। अपने पूरे शिल्प में यह आम बहुत प्रभावित करता था। एक बात जो बार-बार याद आ रही कि इन बाग़ों का पूरा विन्यास अपने पूर्वजों को याद करने के लिए ही बना हुआ था। किसी पेड़ को आप नहीं कह सकते थे कि यह ठीक-ठीक कब का है, बातचीत में पता चलता कि “फलाने काका एक दिन बतावत रहेन की पाही पर वाले बाबू जी के बाबा उनकरे पैदा होय पे लगाये रहेन इ पेड़वा”। पूर्वजों को याद करने का एक ज़रिया भी थे यह बाग़।
बात बाग़ों की रखवाली की करें तो रखवाली भी बस तब तक होती जब तक पेड़ पर आम बचे रहते। इस रखवाली की ज़िम्मेदारी घर के बड़े बुज़ुर्गों की रहती, दो महीना उनका खटिया बिस्तरा वहीं पहुँच जाता। एक छोटी-सी कुटिया नुमा झोपड़ी भी छा दी जाती और चार बाँस लगाकर उसको खड़ा कर दिया जाता। घर से खाना पहुँचाने की व्यवस्था भी हो जाती। उस आदमी की एक बड़ी ज़िम्मेदारी थी, ध्यान देना उस आवाज़ का, जो आम पक के गिरने से होती थी। बिल्कुल शब्दभेदी बाण के मकैनिज्म की तरह उस पेड़ के नीचे पहुँच कर उसको सुरक्षित कर लेना। जब हर एक चीज़ प्लास्टिक नहीं बनी होती थी, तब लोगों के यहाँ बाल्टी लोहे की आती जो बहुत भारी होती थी। गाँव में मार होते समय—एक-दो लोगों की खोपड़ी उस बाल्टी से ज़रूर फूटती थी। बाग़ में वह गिरा हुआ आम पानी भरी बाल्टी में रख दिया जाता और ऐसे रखते-रखते वह बाल्टी भर जाती। फिर उन आमों का बँटवारा होता और सबके यहाँ वे भेज दिए जाते।
धीरे-धीरे बाग़ों की जगह बगीचे हुए, बगीचे लॉन में बदले, अब गार्डेन और बालकनी का दौर है। अब तो बाग़ का ज़िक्र हदबंदी, मेडबंदी और चकबंदी के संदर्भ में ही सुनाई देता है। पूर्वजों के साथ-साथ उनके लगाए पेड़ भी अब स्मृति का हिस्सा होते जा रहे, बाग़ों का पूरा समाजशास्त्र बदल चुका है, बाग़ अब धीरे-धीरे प्लॉट में तब्दील हो रहे हैं। भला हो एन जी टी का जिसने ईंट-भट्टों पर थोड़ा लगाम लगाकर बचे हुए पेड़ों को बचाने की कसर बचा रखी है। बाघों को तो हमने बचा लिया, अब बाग़ों को भी बचाना होगा।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
25 अक्तूबर 2025
लोलिता के लेखक नाबोकोव साहित्य-शिक्षक के रूप में
हमारे यहाँ अनेक लेखक हैं, जो अध्यापन करते हैं। अनेक ऐसे छात्र होंगे, जिन्होंने क्लास में बैठकर उनके लेक्चरों के नोट्स लिए होंगे। परीक्षोपयोगी महत्त्व तो उनका अवश्य होगा—किंतु वह तो उन शिक्षकों का भी
06 अक्तूबर 2025
अगम बहै दरियाव, पाँड़े! सुगम अहै मरि जाव
एक पहलवान कुछ न समझते हुए भी पाँड़े बाबा का मुँह ताकने लगे तो उन्होंने समझाया : अपने धर्म की व्यवस्था के अनुसार मरने के तेरह दिन बाद तक, जब तक तेरही नहीं हो जाती, जीव मुक्त रहता है। फिर कहीं न
27 अक्तूबर 2025
विनोद कुमार शुक्ल से दूसरी बार मिलना
दादा (विनोद कुमार शुक्ल) से दुबारा मिलना ऐसा है, जैसे किसी राह भूले पंछी का उस विशाल बरगद के पेड़ पर वापस लौट आना—जिसकी डालियों पर फुदक-फुदक कर उसने उड़ना सीखा था। विकुशु को अपने सामने देखना जादू है।
31 अक्तूबर 2025
सिट्रीज़ीन : ज़िक्र उस परी-वश का और फिर बयाँ अपना
सिट्रीज़ीन—वह ज्ञान के युग में विचारों की तरह अराजक नहीं है, बल्कि वह विचारों को क्षीण करती है। वह उदास और अनमना कर राह भुला देती है। उसकी अंतर्वस्तु में आदमी को सुस्त और खिन्न करने तत्त्व हैं। उसके स
18 अक्तूबर 2025
झाँसी-प्रशस्ति : जब थक जाओ तो आ जाना
मेरा जन्म झाँसी में हुआ। लोग जन्मभूमि को बहुत मानते हैं। संस्कृति हमें यही सिखाती है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, इस बात को बचपन से ही रटाया जाता है। पर क्या जन्म होने मात्र से कोई शहर अपना ह